आरक्षण की पलायनवादी राजनीति

गूजरों को जनजाति में शामिल किए जाने की मांग को लेकर उठा तूफ़ान अब शांत हो गया है. गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और राजस्थान सरकार के बीच समझौता हो गया है. समझौते का मतलब यह नहीं है कि कोई फैसला हो गया है. बस इतना हुआ है कि एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन का आश्वासन आंदोलनकारियों को दे दिया गया है. अब यह समिति पहले तो तीन महीने तक स्थितियों का अध्ययन करेगी और फिर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी. इसके बाद सरकार उस पर विचार करेगी, बहस-मुबाहिसे होंगे, विधानसभा और संसद से एक-दो बार वाकआउट आदि का नाटक होगा. इतने में चुनाव आ जाएँगे और यह सरकार चली जाएगी. जैसी कि भारत में परम्परा सी बन गयी है, सभी सरकारें जानती हैं कि जैसी उनकी करतूतें रही हैं उस हिसाब से जनता उन्हें तुरंत दुबारा सत्ता सौपने की बेवकूफी तो कर नहीं सकती है.
अब यह मुश्किल अगली सरकार की होगी. खुदा ना खास्ता अगर कहीँ दुबारा सत्ता में तुरंत वापसी हो भी गयी तो भी इतनी चिन्ता की कोई बात इसमें नहीं है. आखिर समस्या हल तो होनी नहीं है, लिहाजा फिर किसी तरह टाल दीं जाएगी. कोई न कोई नया बहाना तब तक जरूर तलाश लिया जाएगा. चाहे तो कोई नया आश्वासन दे दिया जाएगा, या कोई नया सपना दिखा दिया जाएगा, या फिर उन्हें जनजाति का दर्जा ही दे दिया जाएगा. कौन सा इससे विधायकों-मंत्रियों का कोई व्यक्तिगत नुकसान होने वाला है या सरकार का कुछ घट जाने वाला है? जिन्हे अनुसूचित जाति या जनजाति का दर्जा दे दिया गया है क्या उन सबको सरकारी नौकरियाँ मिल गयी हैं या सबके बच्चों की पढ़ाई हो गयी है? नहीं, ऐसा कुछ भी न तो हुआ है और न निकट भविष्य में होने जा रहा है.
हुआ सिर्फ यह है कि हमारे राजनेता लोगों की समस्याएं हल करने के बजाय उन्हें सिर्फ बरगलाते चले आ रहे हैं. समस्याएँ हल करने में उनकी कोई दिलचस्पी न कभी थी, न है और न कभी होगी ही. सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की, चाहे कम्युनिस्टों की, या फिर किसी और की. जनता के हितों की चिन्ता भारतीय राजनेताओं को सिर्फ तभी तक होती है जब तक उन्हें सत्ता हासिल नहीं हो जाती. सत्ता हासिल होते ही उनकी चिन्ता का केंद्रबिन्दु उनकी कुर्सी हो जाती है और उसकी धुरी केवल पूंजीपतियों के इर्द-गिर्द घूमने लगती है. जनता के संदर्भ में उनकी चिन्ता सिर्फ यह होती है कि उसे कैसे बाँटा जाए. कभी जाति के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर और कभी वर्ग के नाम पर. कभी हिंदू-मुसलमान लड़ते हैं तो कभी अगडे-पिछड़े और कभी पिछड़े-पिछड़े या अगडे-अगडे भी. आम जनता की स्थिति इसमें हमेशा तरबूज जैसी होती है और खास लोगों यानी राजनेताओं की हैसियत हमेशा चाक़ू वाली ही रहती है. चक्काजाम के चलते आना-जाना रुकता है. दिहाडी मारी जाती, बच्चों की पढाई या बीमार की दवाई मारी जाती है. सारी मुसीबतों का शिकार आम आदमी ही होता है. बडे लोग अपनी सभी जरूरतों को पूरा करने का इंतजाम पहले से किए रहते हैं.
जहाँ तक सवाल आम आदमी का है उसको तो किसी खास वर्ग में शामिल करके भी वे हलाल ही करते हैं और न करके भी. आरक्षण देकर तो वे हमें हलाल करते ही हैं, न देकर भी वही करते हैं. ठीक यही स्थिति तुष्टीकरण के मामले में भी है. उनका इरादा जनता की समस्याओं का समाधान नहीं, उसे हलाल करना होता है. अगर समस्याओं का समाधान उन्हें करना होता तो बजाय आरक्षण के वे रोजगार के अवसर बढ़ाते. लेकिन रोजगार के अवसर वह लगातार घटाते जा रहे हैं. निजी क्षेत्र पर आरक्षण के लिए दबाव बनाया जा रहा है और श्रम कानूनों की ऐसी-तैसी की जा रही है. यह सब तब हो रहा है जब सरकार कम्युनिस्टों के दम पर चल रही है. भारतीय कम्युनिस्टों के इरादे साफ जाहिर कर देने के लिए सिर्फ इतना काफी है कि वे यह सब बखूबी समझते हुए भी चुप हैं, बिल्कुल चुप. इनकी चुप्पी अपनी चुप्पी के लिए ही कुख्यात नरसिंह राव की चुप्पी से बहुत ज्यादा खतरनाक है. क्योंकि ये कभी-कभी गीदड़भभकी भी देते हैं. हालांकि इन्हें भी पता है कि कुछ नहीं करना है और सरकार चलाने वाले भी जानते हैं कि कुछ नहीं होना है. इन्हें सरकार में रहने की मलाई काटनी है और उन्हें सरकार चलाने की.
ऐसा नहीं है कि यह बात केवल कम्युनिस्टों और कांग्रेसियों के साथ ही हो. सभी पार्टियों का एक ही जैसा हाल है. याद करिये सन १९९० जब वी पी सिंह मंडल कमीशन लेकर आए थे. इस उम्मीद में कि प्रधानमंत्री की कुर्सी आगे से उनके खानदान के लिए ही आरक्षित हो जाए. बिल्कुल वैसे ही जैसे नेहरू परिवार उसे अपनी पुश्तैनी संपदा मानता है. निजी महत्वाकांक्षा के लिए देशहित की बलि कैसे दीं जाती है, इसका संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन से बड़ा उदाहरण नही हो सकता. उस समय पूरा देश जल उठा था. दिल्ली तो बुरी तरह धधक रही थी. बच्चे और नौजवान आत्मदाह करने पर तुले थे. देश की तमाम प्रतिभाएं खुद अपनी जान दे रही थीं. और यह तथाकथित कवि-पेंटर चैन की बांसुरी बजा रहा था. भारत में उस समय जातिवाद मृत्युशैया पर पड़ा था, जिसके जिस्म में वी पी सिंह ने नए प्राण फूंक दिए. उस समय उनकी सरकार कम्युनिस्टों और भाजपाइयों दोनों के सहयोग से चल रही थी. इनमें भाजपाइयों की भूमिका पर तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन वामपंथियों की नपुंसक चुप्पी हर किसी के लिए आश्चर्यजनक थी. वह भी अपने सिद्धांतों के विपरीत मुद्दे पर.
आम तौर पर देखा यह जाता है कि भारतीय राजनेता सत्ता हासिल करने के लिए सारे सिद्धांतों को किनारे कर गठबंधन कर लेते हैं. आगे कुर्सी बचाए रखने के लिए भी वे वही सब करते रहते है जो उनके तथाकथित सिद्धांतों के विपरीत होता है. आख़िर क्यों ? इसका एक अच्छा जवाब अपने एक कार्टून में दिया है जगजीत राणा ने. दैनिक जागरण के पहले ही पन्ने पर कार्टून में गूजरों के मुद्दे पर बिठाये गए आयोग के संबंध में टिप्पणी है, "पहले आयोग क्यों नहीं बिठाते कि ऐसा वादा किया जा सकता है या नहीं". असल में यहाँ सारे आयोग बिठाये ही जाते हैं या तो मुद्दे को टालने के लिए या फिर अपने मनमुताबिक परिणाम निकालने के लिए. जमीनी मुद्दों से पलायन भारतीय राजनेताओं की मूल प्रवृत्ति है. क्योंकि जनता के सुखों के संदर्भ में इनके भीतर कोई इच्छाशक्ति ही नहीं है. इसलिए इनकी कुल राजनीति केवल जनता को उसके वास्तविक मुद्दों से भटकाने की है. पर सवाल यह है कि पलायन की यह राजनीति कितने दिन चलेगी?
जनता की हताशा जैसे अभी छोटे-छोटे ग़ुस्से के रुप में सामने आ रही है, वैसे ही यह एक दिन संगठित विद्रोह का रुप भी ले सकती है. यह विद्रोह ऐसा नहीं होगा जिसका नेतृत्व किसी दलाल या नपुंसक के हाथ में चला जाएगा. अब भारत की जनता ऐसा इसलिए नहीं होने देगी क्योंकि आजादी की लड़ाई और उसके बाद के कई संघर्षों के हश्र वह देख चुकी है. तब क्या होगा मंडल, कमंडल, आरक्षण और तुष्टीकरण का? सच से पलायन कितने दिनों तक चलेगा? पहले छात्रों, फिर डॉक्टरों और अब गूजरों का ग़ुस्सा राजनेताओं को यही संकेत दे रहा है कि संभल जाओ. तुम्हारे लाख पैंतरों के बावजूद सत्ता पर काबिज होना हमें आता है और सच से जितना पीछा छुडाओगे, यह उतना ही तुम्हारा पीछा करेगा. आरक्षण के नाम पर बहकाने की कोशिशों के दिन अब लद गए. जागो, दुनिया देखो. शिक्षा और रोजगार, जो हमारा मौलिक अधिकार है ही, इन्हें मौलिक अधिकार की तरह हम सबको उपलब्ध कराओ. बांटो और राज करो की नीति अब बहुत दिन नहीं चलेगी. चिरनिद्रालीन और महापलायनवादी भारतीय राजनेताओं की समझ में यह सच्चाई आयी या नहीं, यह समय बताएगा.
इष्ट देव सांकृत्यायन
अब यह मुश्किल अगली सरकार की होगी. खुदा ना खास्ता अगर कहीँ दुबारा सत्ता में तुरंत वापसी हो भी गयी तो भी इतनी चिन्ता की कोई बात इसमें नहीं है. आखिर समस्या हल तो होनी नहीं है, लिहाजा फिर किसी तरह टाल दीं जाएगी. कोई न कोई नया बहाना तब तक जरूर तलाश लिया जाएगा. चाहे तो कोई नया आश्वासन दे दिया जाएगा, या कोई नया सपना दिखा दिया जाएगा, या फिर उन्हें जनजाति का दर्जा ही दे दिया जाएगा. कौन सा इससे विधायकों-मंत्रियों का कोई व्यक्तिगत नुकसान होने वाला है या सरकार का कुछ घट जाने वाला है? जिन्हे अनुसूचित जाति या जनजाति का दर्जा दे दिया गया है क्या उन सबको सरकारी नौकरियाँ मिल गयी हैं या सबके बच्चों की पढ़ाई हो गयी है? नहीं, ऐसा कुछ भी न तो हुआ है और न निकट भविष्य में होने जा रहा है.
हुआ सिर्फ यह है कि हमारे राजनेता लोगों की समस्याएं हल करने के बजाय उन्हें सिर्फ बरगलाते चले आ रहे हैं. समस्याएँ हल करने में उनकी कोई दिलचस्पी न कभी थी, न है और न कभी होगी ही. सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की, चाहे कम्युनिस्टों की, या फिर किसी और की. जनता के हितों की चिन्ता भारतीय राजनेताओं को सिर्फ तभी तक होती है जब तक उन्हें सत्ता हासिल नहीं हो जाती. सत्ता हासिल होते ही उनकी चिन्ता का केंद्रबिन्दु उनकी कुर्सी हो जाती है और उसकी धुरी केवल पूंजीपतियों के इर्द-गिर्द घूमने लगती है. जनता के संदर्भ में उनकी चिन्ता सिर्फ यह होती है कि उसे कैसे बाँटा जाए. कभी जाति के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर और कभी वर्ग के नाम पर. कभी हिंदू-मुसलमान लड़ते हैं तो कभी अगडे-पिछड़े और कभी पिछड़े-पिछड़े या अगडे-अगडे भी. आम जनता की स्थिति इसमें हमेशा तरबूज जैसी होती है और खास लोगों यानी राजनेताओं की हैसियत हमेशा चाक़ू वाली ही रहती है. चक्काजाम के चलते आना-जाना रुकता है. दिहाडी मारी जाती, बच्चों की पढाई या बीमार की दवाई मारी जाती है. सारी मुसीबतों का शिकार आम आदमी ही होता है. बडे लोग अपनी सभी जरूरतों को पूरा करने का इंतजाम पहले से किए रहते हैं.
जहाँ तक सवाल आम आदमी का है उसको तो किसी खास वर्ग में शामिल करके भी वे हलाल ही करते हैं और न करके भी. आरक्षण देकर तो वे हमें हलाल करते ही हैं, न देकर भी वही करते हैं. ठीक यही स्थिति तुष्टीकरण के मामले में भी है. उनका इरादा जनता की समस्याओं का समाधान नहीं, उसे हलाल करना होता है. अगर समस्याओं का समाधान उन्हें करना होता तो बजाय आरक्षण के वे रोजगार के अवसर बढ़ाते. लेकिन रोजगार के अवसर वह लगातार घटाते जा रहे हैं. निजी क्षेत्र पर आरक्षण के लिए दबाव बनाया जा रहा है और श्रम कानूनों की ऐसी-तैसी की जा रही है. यह सब तब हो रहा है जब सरकार कम्युनिस्टों के दम पर चल रही है. भारतीय कम्युनिस्टों के इरादे साफ जाहिर कर देने के लिए सिर्फ इतना काफी है कि वे यह सब बखूबी समझते हुए भी चुप हैं, बिल्कुल चुप. इनकी चुप्पी अपनी चुप्पी के लिए ही कुख्यात नरसिंह राव की चुप्पी से बहुत ज्यादा खतरनाक है. क्योंकि ये कभी-कभी गीदड़भभकी भी देते हैं. हालांकि इन्हें भी पता है कि कुछ नहीं करना है और सरकार चलाने वाले भी जानते हैं कि कुछ नहीं होना है. इन्हें सरकार में रहने की मलाई काटनी है और उन्हें सरकार चलाने की.
ऐसा नहीं है कि यह बात केवल कम्युनिस्टों और कांग्रेसियों के साथ ही हो. सभी पार्टियों का एक ही जैसा हाल है. याद करिये सन १९९० जब वी पी सिंह मंडल कमीशन लेकर आए थे. इस उम्मीद में कि प्रधानमंत्री की कुर्सी आगे से उनके खानदान के लिए ही आरक्षित हो जाए. बिल्कुल वैसे ही जैसे नेहरू परिवार उसे अपनी पुश्तैनी संपदा मानता है. निजी महत्वाकांक्षा के लिए देशहित की बलि कैसे दीं जाती है, इसका संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन से बड़ा उदाहरण नही हो सकता. उस समय पूरा देश जल उठा था. दिल्ली तो बुरी तरह धधक रही थी. बच्चे और नौजवान आत्मदाह करने पर तुले थे. देश की तमाम प्रतिभाएं खुद अपनी जान दे रही थीं. और यह तथाकथित कवि-पेंटर चैन की बांसुरी बजा रहा था. भारत में उस समय जातिवाद मृत्युशैया पर पड़ा था, जिसके जिस्म में वी पी सिंह ने नए प्राण फूंक दिए. उस समय उनकी सरकार कम्युनिस्टों और भाजपाइयों दोनों के सहयोग से चल रही थी. इनमें भाजपाइयों की भूमिका पर तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन वामपंथियों की नपुंसक चुप्पी हर किसी के लिए आश्चर्यजनक थी. वह भी अपने सिद्धांतों के विपरीत मुद्दे पर.
आम तौर पर देखा यह जाता है कि भारतीय राजनेता सत्ता हासिल करने के लिए सारे सिद्धांतों को किनारे कर गठबंधन कर लेते हैं. आगे कुर्सी बचाए रखने के लिए भी वे वही सब करते रहते है जो उनके तथाकथित सिद्धांतों के विपरीत होता है. आख़िर क्यों ? इसका एक अच्छा जवाब अपने एक कार्टून में दिया है जगजीत राणा ने. दैनिक जागरण के पहले ही पन्ने पर कार्टून में गूजरों के मुद्दे पर बिठाये गए आयोग के संबंध में टिप्पणी है, "पहले आयोग क्यों नहीं बिठाते कि ऐसा वादा किया जा सकता है या नहीं". असल में यहाँ सारे आयोग बिठाये ही जाते हैं या तो मुद्दे को टालने के लिए या फिर अपने मनमुताबिक परिणाम निकालने के लिए. जमीनी मुद्दों से पलायन भारतीय राजनेताओं की मूल प्रवृत्ति है. क्योंकि जनता के सुखों के संदर्भ में इनके भीतर कोई इच्छाशक्ति ही नहीं है. इसलिए इनकी कुल राजनीति केवल जनता को उसके वास्तविक मुद्दों से भटकाने की है. पर सवाल यह है कि पलायन की यह राजनीति कितने दिन चलेगी?
जनता की हताशा जैसे अभी छोटे-छोटे ग़ुस्से के रुप में सामने आ रही है, वैसे ही यह एक दिन संगठित विद्रोह का रुप भी ले सकती है. यह विद्रोह ऐसा नहीं होगा जिसका नेतृत्व किसी दलाल या नपुंसक के हाथ में चला जाएगा. अब भारत की जनता ऐसा इसलिए नहीं होने देगी क्योंकि आजादी की लड़ाई और उसके बाद के कई संघर्षों के हश्र वह देख चुकी है. तब क्या होगा मंडल, कमंडल, आरक्षण और तुष्टीकरण का? सच से पलायन कितने दिनों तक चलेगा? पहले छात्रों, फिर डॉक्टरों और अब गूजरों का ग़ुस्सा राजनेताओं को यही संकेत दे रहा है कि संभल जाओ. तुम्हारे लाख पैंतरों के बावजूद सत्ता पर काबिज होना हमें आता है और सच से जितना पीछा छुडाओगे, यह उतना ही तुम्हारा पीछा करेगा. आरक्षण के नाम पर बहकाने की कोशिशों के दिन अब लद गए. जागो, दुनिया देखो. शिक्षा और रोजगार, जो हमारा मौलिक अधिकार है ही, इन्हें मौलिक अधिकार की तरह हम सबको उपलब्ध कराओ. बांटो और राज करो की नीति अब बहुत दिन नहीं चलेगी. चिरनिद्रालीन और महापलायनवादी भारतीय राजनेताओं की समझ में यह सच्चाई आयी या नहीं, यह समय बताएगा.
इष्ट देव सांकृत्यायन




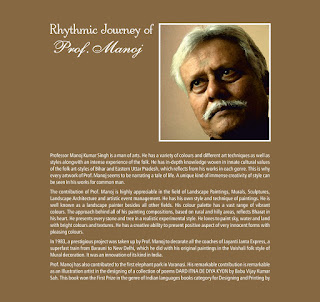


BRILLIANT !!!
ReplyDeleteThe "Heart of the matter" has been defined.