असली फुरसतिया शिरी लालू जी
अभी दो दिन पहले ही एक पोस्ट पढा था. मसिजीवी भाई का. मन बना था कि पहले उसी पर लिखूंगा. उन्होने बात गांवों को शहरों में बदले जाने के समर्थन में की है. जिस लेख से प्रभावित होकर उन्होने इसका समर्थन किया है अतानु का वह लेख भी पढ़ लिया. तर्क तो मेरे पास ख़ूब हैं, लेकिन इस पर बाद में लिखूंगा. पहले ग़ुस्सा निकल जाए तब, ताकि अगले के साथ कम से कम अन्याय तो न हो! अहा ग्राम्य जीवन भी ख़ूब है, की जमीनी हकीकत मैं बहुत करीब से जानता हूँ. जिस गाँव में मैं पला बढ़ा हूँ वह बाढ और सूखे से ग्रस्त तो नहीं है, लेकिन सरकारी और राजनीतिक लूट-खसोट का जो तांडव वहां मचा है और उसके चलते गाँव के भीतर की सुख शांति जिस तरह छिन्न-भिन्न हो रही है, उसे जानते हुए भी ग्राम्य जीवन के प्रति किसी का आकर्षण बचा रह जाए, यह लगभग नामुमकिन है. इससे भी ज्यादा भयावह स्थिति उस गाँव की है जहाँ से हमारे पूर्वज आए और आकर महराजगंज (तब गोरखपुर) जिले के बैकुंठपुर गाँव में बसे थे. वह गाँव मलांव है. यही वह गाँव है जहाँ से राहुल जी के पूर्वज आजमगढ़ चले गए थे और वहां कनैला गाँव में बस गए थे. मलांव अभी भी गोरखपुर जिले में ही है और हर साल बाढ वहां जैसी तबाही मचाती है और साथ ही सरकारी तंत्र बाढ के नाम पर जैसी लूट-खसोट मचाता है उसे देखने के बाद तो कोई भी यही कहेगा कि इस देश से गाँव नेस्तनाबूद कर दिए जाने चाहिए. लेकिन मैं फिर भी ऐसा नहीं कहूँगा, पर इस मुद्दे पर पूरी बात बाद में.
अभी फ़िलहाल ग्राम्य जीवन के बजाय रेल जीवन पर .... अहा रेल जीवन भी क्या ख़ूब है! लालू जी इसे फायदे में चाहे जितना दिखाएँ और उनके फायदे नुकसान के आंकड़ों की असलियत चाहे जो हो, पर वह उसे यात्री के चलने लायक अभी भी नहीं बना सके हैं. शायद कभी भी .....
यह बात है १९-२० जून की है. पूरी रात कानपुर रेलवे स्टेशन पर टहलते गुज़री. जो ट्रेन रात साढ़े नौ बजे आनी थी वह भोर में करीब चार बजे आयी. पहले से पता रहा होता कि रेलिया इतनी बैरी है तो मैं वहाँ वरिष्ठ कथाकार राजेंद्र राव जी के घर ही चला गया होता. एक आत्मीय बडे भाई के साथ का सुख थोडा और ले लिया होता. या फिर तुरन्त ही मिले और आत्मीय हो गए भाई फुरसतिया जीं के साथ थोडा और समय गुजर लिया होता तो यह संकट नहीं आता. अगर रात जागते भी बीती होती तो भी कष्ट नहीं होता क्योंकि बोर तो न होना पड़ता. पर क्या करिएगा? मेरे एक लतीफेबाज पत्रकार मित्र विनोद बंधु, जो इन दिनों शायद पटना में कहीँ पाए जाते होंगे का कहना है कि भारत की रेल न तो ड्राइवर चलाता है न गार्ड चलाता है, इसे तो बस गाड चलाता है. मुझे मनाना पड़ा कि किस्मत में यही लिखा था. बहरहाल यह भी किस्मत ही बात थी जिसके चलते भाई फुरसतिया जी, यानी ब्लोग बाबा अनूप शुक्ल जीं से मेरी मुलाक़ात हो गयी और इसमें भी जितनी बड़ी भूमिका हमारे संस्थान यानी दैनिक जागरण ने निभाई, रेल की भूमिका को उससे रत्ती भर भी कम करके नहीं आका जा सकता है। यह रेल ही थी जिसने यह संयोग बनाया कि हमारी बैठक शुक्लाजी के साथ हो गयी। हुआ यह कि हमारी ट्रेन इधर यानी दिल्ली से ही कानपुर तक पहुंचते-पहुंचते एक-डेढ़ घंटे देर हो चुकी थी। जैसे-तैसे भागते-भागते कार्यालय पहुंचा तो पता चला कि समूह अध्यक्ष योगेंद्र मोहन जी कहीँ और चले गए. अब वह शाम को आएंगे. ५ बजे. मीटिंग भी तभी होगी.
सवाल उठा कि तब क्या हो? अब यह तीन घंटे कैसे और कहॉ गुजारे जाएँ. राव साहब ने तय किया लक्ष्मी देवी ललित कला संस्थान चला जाए. वहीं कुछ खा भी लिया जाएगा, आराम भी कर लेंगे और कुछ मुद्दों पर चर्चा भी हो जाएगी. इसके पहले कि हम संस्थान पहुंचते रास्ते में गाडी में ही साहित्य के इन्तेर्नेतिया मध्यम पर चर्चा शुरू हो गयी. इसी चर्चा के क्रम में विनोद जी ने बताया कि हिंदी mein ब्लोगिन्ग के दादा अनूप शुक्ल तो यही रहते हैं. मैंने कहा अच्छा , वह बोले हाँ. विनोद ने पूछा मिलना चाहेंगे, मैंने कहा भाई मिलवाइए. संस्थान पहुंच कर फोना-फानी हुई और थोडी ही देर में शुक्ल जी हमारे सामने थे. फुरसतिया से अपना परिचय तो पुराना था. श्रीलाल शुक्ल जी के ब्लोग रागदरबारी के माध्यम से. श्रीलाल जी व्यक्तित्व पर भाई फुरसतिया ने जैसा लिखा है, वह फुर्सत में ही लिखा जा सकता है. फुर्सत में ही एक कृती व्यक्तित्व को उस तरह से समझना भी संभव है.
वह लेख पढने के बाद मैंने उनके कई और लेख भी पढे, पर उसका असर मन पर से गया नहीं. जाने क्यों?चर्चा चली तो इलाहाबाद भी चली गयी और फिर पुरानी एकता के सूत्रभी
जुड़ गए. खैर, ख़ूब गुज़री जब मिल बैठे दीवाने दो. पर मेरा दुर्भाग्य देखिए जिस समय मैं कानपुर स्टेशन पर परकटे पंछी की तरह अकेले तड़फड़ा रहा था और ती वी चैनलों पर दिखाए जाने वाले प्रेतात्माओं की तरह भटक रहा था तब किसी भी तरफ से यह आवाज नहीं आयी कैश सेहरा में अकेला है, मुझे जाने दो. बहरहाल यह तो बाद की बात है. उसके पहले हमारी लम्बी बातचीत हुई. साहित्य, संस्कृति, समाज, राजनीति; हर जगह जो भ्रष्टाचार और कदाचार व्याप्त है वह और उसमें ब्लोगिये जो सार्थक भूमिका निभा सकते हैं उसकी संभावनाएं ........ जो कुछ... तकनीकी दिक्कतें मुझे ब्लागियाने के दौरान झेलनी पडती हैं उन पर भी चर्चा हुई.
अभी हमारी बातचीत पूरी भी नहीं हुई थी कि मीटिंग का समय हो गया और हम संस्थान से कार्यालय की ओर कूच कर गए. ढाई-तीन घंटे की बैठक के बाद सवाल उठा कि अब। राव साहब चाहते थे कि मैं उनके घर की ओर चलूँ और मुझे ट्रेन पकड़नी थी। अव्वल तो बहुत थोड़े ही समय में राव साहब से जैसी आत्मीयता हुई, कम ही लोगों से हो पाती है। जो सहज और पारिवारिक व्यवहार उनका है, वह उनके साथ-साथ कानपुर से लगाव लगाने लगता है. इसलिए जाना तो मैं चाहता था, पर रेल का टाइम हो गया था और मैं उसकी अनदेखी नहीं कर सकता था. लिहाजा चलना पड़ा. कार्यालय से संस्थान तक फिर भी हम लोग साथ-साथ आए और वहाँ थोड़ी देर तक ठहरे भी. इसके बाद पौने नौ होते ही मैं स्टेशन की ओर चल पड़ा. ठीक सवा नौ बजे मैं वहाँ पहुंच भी गया.
असली त्रासदी यहीं से शुरू हुई. रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद. मालूम हुआ कि जिस रेल से मुझे जाना है वह दो घंटे विलंब से आ रही है.थोड़ी देर तक इधर-उधर टहलने के बाद मैं वेटिंग रूम में चला गया और वहीं एक खाली पडी कुर्सी पर कब्जा जमा कर नरेन्द्र मोहन जी की नई आई किताब 'संस्कृति और राष्ट्रवाद' पढने लगा. मैं पढने में मगन हो गया तो फिर रेल और समय की फिक्र भी जाती रही. हाँ कान ट्रेनों के आवागमन संबंधी घोषणाओं पर जरूर लगे हुए थे. करीब एक घंटे यानी ११ बजे तक मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं थी. ११ बजे यह घोषणा हुई कि गाडी संख्या ४१५ अपने निर्धारित समय से पौने तीन घंटे देर है. तो भी मैंने कहा कोई बात नहीं. अब १२ बजे तक आराम से पढेंगे. इसके बाद ही उठेंगे. मैं पढने में लगा रहा. १२ बजे फिर घोषणा हुई कि यह ट्रेन अब चार घंटे विलंब से आ रही है. लेकिन साहब चार घंटे विलंब होने यानी रात के डेढ़ बजने तक जब ट्रेन नंबर ४१५ के संबंध में कोई और घोषणा नहीं हुई तो मुझे लगा कि यह क्या ट्रेन नंबर ४२० हो गई.
आख़िर मैं वहाँ से उठा और इन्क्वायरी काउंटर गया. वहाँ मालूम हुआ साहब अभी कोई सूचना नहीं है, हाँ आएगी वह प्लेटफार्म नंबर दो पर ही. मैंने सोचा जब कोई सूचना नहीं है तो क्या भरोसा, अचानक आ ही जाए? बेहतर यही है कि प्लेटफार्म नंबर दो पर ही चला जाए. वहाँ हमारे जैसे सैकड़ों रेलपीडित अतृप्त आत्माओं की तरह इधर-उधर भटक रहे थे. सबका दर्द यही था कि रेल को दो-चार-छः नहीं चौबीस घंटे देर से भी आना हो तो कोई बात नहीं, पर हाकिमान यह बता तो दें कि कितनी देर लगेगी.
इस गलतबयानी का नतीजा यह होता है कि तमाम यात्री आ कर स्टेशन पर अनायास टपकते रहते हैं. न तो उनका कोई पुरसाहाल होता है और न कोई उद्देश्य ही हल होता है. इंतज़ार की इस लें में ऐसे मरीज भी हो सकते हैं जिनके लिए इधर-उधर भटकना नुकसानदेह हो सकता है. यूँ तो यह स्वस्थ आदमी के लिए भी नुकसानदेह है. और यात्रियों की छोड़िये, यह तो रेल के लिए भी नुकसानदेह है. इसे गलतबयानी या सही आकलन की क्षमता का अभाव, जो भी कह लें, का ही नतीजा है जो प्लेट्फार्मों पर अनावश्यक भीड़ हमेशा दिखाई देती है. ठीक समय मालूम न होने के नाते यात्रियों को वहाँ भटकना पड़ता है. और कई यात्रियों के साथ उन्हें पहुँचाने आए लोगों को भी भटकना पङता है. बेमतलब ही भीड़ बढती जाती है और शोर बढ़ता जाता है.
इस भीड़ का फायदा अराजक तत्त्व उठाते हैं. ऎसी ही स्थितियों में कभी कहीँ विस्फोट होता है तो कहीँ भगदड़ मचाती है और इस सबमें सैकड़ों लोगों की जानें जाती हैं. रेल कुछ न करे, केवल समय से सही सूचनाओं की लेन-देन का इंतजाम भर बना ले तो न केवल रेल, बल्कि यात्रियों और देश की भी आधी समस्यायें हल हो जाएंगी. बहरहाल साहब, अपने राम वहाँ घूमते रहे. चूंकि ठसाठस भरे प्लेटफार्म पर बैठाने के लिए कोई जगह थी नहीं, लिहाजा पढाई भी नहीं की जा सकती थी. मजबूरन इधर-उधर घूमते रहे. रात के साढ़े तीन बज गए. इस बीच कई दूसरी ट्रेनें उसी प्लेटफार्म से आईं-गईं. पर ४१५ के बारे में कोई घोषणा तक नहीं हुई.
घोषणा हुई साढ़े तीन बजे और वह भी सिर्फ इतनी कि अब वह प्लेटफार्म नंबर २ नहीं १ पर आएगी. इस पर जो कुछ लोग परिवार समेट आकर दो नंबर प्लेटफार्म पर बैठ चुके थे और जिनके साथ ज्यादा सामान भी थे उन्होने रेल के अफसरों-कर्मचारियों से अपने निकट संबंधों के दावे शुरू कर दिए. काश बिना किसी माइक के की जाने वाली यात्रियों की ये प्रीतिकर घोषणाएँ रेल की व्यवस्था के कान तक पहुंच पाते. आखिरकार वह चिर-प्रतीक्षित शुभ मुहूर्त आ ही गया जब रेल आ गयी. भोर के चार बजे. सारे यात्रियों के साथ मैं भी भागा और जैसे-तैसे अपना डिब्बा तलाश कर उसमें लदा. लद कर व्यवस्थित होते ही एक यात्री ने अपने साथी से सवाल किया जब देर से आयी है तो पहुँचेगी भी देर ही से? 'अरे आ गयी यही क्या कम है, जो अब पहुँचाने की भी सोचने लगे? देर की बात छोड़ दो. पहुंच जाओ बस यही मनाओ. यूँ तो रेल में तब तक बैठो ही नहीं जब तक फुरसतिए न हो. भारतीय रेल फुरसतियों की ही है.' जबकि मैं हतबुद्धि, सोच रहा था कि फुरसतिया जी को तो मैं छोड़ आया था. यहाँ आकर पता चला कि भारत की तो रेल ही उनकी ही है. मुझे लगा कि शायद यह ठीक कह रहे हैं. वर्त्तमान रेलमंत्री, यानी लालू जी अपने बारे में लीक से हट कर काम यानी प्रयोग करने के प्रचार कराने में माहिर हैं. जबकि अपने फुरसतिया भाई लीक से हटकर प्रयोग करने में माहिर हैं और वह भी बिना बताए. अरे भाई, लालू जी सुना आपने, छोड़ न दीजिए सिंहासन और नईं तो मान लीजिए कि आप ही फुरसतिया हैं. बेचारे रेलपीडित तो ऐसा ही मानते हैं.
हतबुद्धि, सोच रहा था कि फुरसतिया जी को तो मैं छोड़ आया था. यहाँ आकर पता चला कि भारत की तो रेल ही उनकी ही है. मुझे लगा कि शायद यह ठीक कह रहे हैं. वर्त्तमान रेलमंत्री, यानी लालू जी अपने बारे में लीक से हट कर काम यानी प्रयोग करने के प्रचार कराने में माहिर हैं. जबकि अपने फुरसतिया भाई लीक से हटकर प्रयोग करने में माहिर हैं और वह भी बिना बताए. अरे भाई, लालू जी सुना आपने, छोड़ न दीजिए सिंहासन और नईं तो मान लीजिए कि आप ही फुरसतिया हैं. बेचारे रेलपीडित तो ऐसा ही मानते हैं.
इष्ट देव सांकृत्यायन
अभी फ़िलहाल ग्राम्य जीवन के बजाय रेल जीवन पर .... अहा रेल जीवन भी क्या ख़ूब है! लालू जी इसे फायदे में चाहे जितना दिखाएँ और उनके फायदे नुकसान के आंकड़ों की असलियत चाहे जो हो, पर वह उसे यात्री के चलने लायक अभी भी नहीं बना सके हैं. शायद कभी भी .....
यह बात है १९-२० जून की है. पूरी रात कानपुर रेलवे स्टेशन पर टहलते गुज़री. जो ट्रेन रात साढ़े नौ बजे आनी थी वह भोर में करीब चार बजे आयी. पहले से पता रहा होता कि रेलिया इतनी बैरी है तो मैं वहाँ वरिष्ठ कथाकार राजेंद्र राव जी के घर ही चला गया होता. एक आत्मीय बडे भाई के साथ का सुख थोडा और ले लिया होता. या फिर तुरन्त ही मिले और आत्मीय हो गए भाई फुरसतिया जीं के साथ थोडा और समय गुजर लिया होता तो यह संकट नहीं आता. अगर रात जागते भी बीती होती तो भी कष्ट नहीं होता क्योंकि बोर तो न होना पड़ता. पर क्या करिएगा? मेरे एक लतीफेबाज पत्रकार मित्र विनोद बंधु, जो इन दिनों शायद पटना में कहीँ पाए जाते होंगे का कहना है कि भारत की रेल न तो ड्राइवर चलाता है न गार्ड चलाता है, इसे तो बस गाड चलाता है. मुझे मनाना पड़ा कि किस्मत में यही लिखा था. बहरहाल यह भी किस्मत ही बात थी जिसके चलते भाई फुरसतिया जी, यानी ब्लोग बाबा अनूप शुक्ल जीं से मेरी मुलाक़ात हो गयी और इसमें भी जितनी बड़ी भूमिका हमारे संस्थान यानी दैनिक जागरण ने निभाई, रेल की भूमिका को उससे रत्ती भर भी कम करके नहीं आका जा सकता है। यह रेल ही थी जिसने यह संयोग बनाया कि हमारी बैठक शुक्लाजी के साथ हो गयी। हुआ यह कि हमारी ट्रेन इधर यानी दिल्ली से ही कानपुर तक पहुंचते-पहुंचते एक-डेढ़ घंटे देर हो चुकी थी। जैसे-तैसे भागते-भागते कार्यालय पहुंचा तो पता चला कि समूह अध्यक्ष योगेंद्र मोहन जी कहीँ और चले गए. अब वह शाम को आएंगे. ५ बजे. मीटिंग भी तभी होगी.
सवाल उठा कि तब क्या हो? अब यह तीन घंटे कैसे और कहॉ गुजारे जाएँ. राव साहब ने तय किया लक्ष्मी देवी ललित कला संस्थान चला जाए. वहीं कुछ खा भी लिया जाएगा, आराम भी कर लेंगे और कुछ मुद्दों पर चर्चा भी हो जाएगी. इसके पहले कि हम संस्थान पहुंचते रास्ते में गाडी में ही साहित्य के इन्तेर्नेतिया मध्यम पर चर्चा शुरू हो गयी. इसी चर्चा के क्रम में विनोद जी ने बताया कि हिंदी mein ब्लोगिन्ग के दादा अनूप शुक्ल तो यही रहते हैं. मैंने कहा अच्छा , वह बोले हाँ. विनोद ने पूछा मिलना चाहेंगे, मैंने कहा भाई मिलवाइए. संस्थान पहुंच कर फोना-फानी हुई और थोडी ही देर में शुक्ल जी हमारे सामने थे. फुरसतिया से अपना परिचय तो पुराना था. श्रीलाल शुक्ल जी के ब्लोग रागदरबारी के माध्यम से. श्रीलाल जी व्यक्तित्व पर भाई फुरसतिया ने जैसा लिखा है, वह फुर्सत में ही लिखा जा सकता है. फुर्सत में ही एक कृती व्यक्तित्व को उस तरह से समझना भी संभव है.
वह लेख पढने के बाद मैंने उनके कई और लेख भी पढे, पर उसका असर मन पर से गया नहीं. जाने क्यों?चर्चा चली तो इलाहाबाद भी चली गयी और फिर पुरानी एकता के सूत्रभी
जुड़ गए. खैर, ख़ूब गुज़री जब मिल बैठे दीवाने दो. पर मेरा दुर्भाग्य देखिए जिस समय मैं कानपुर स्टेशन पर परकटे पंछी की तरह अकेले तड़फड़ा रहा था और ती वी चैनलों पर दिखाए जाने वाले प्रेतात्माओं की तरह भटक रहा था तब किसी भी तरफ से यह आवाज नहीं आयी कैश सेहरा में अकेला है, मुझे जाने दो. बहरहाल यह तो बाद की बात है. उसके पहले हमारी लम्बी बातचीत हुई. साहित्य, संस्कृति, समाज, राजनीति; हर जगह जो भ्रष्टाचार और कदाचार व्याप्त है वह और उसमें ब्लोगिये जो सार्थक भूमिका निभा सकते हैं उसकी संभावनाएं ........ जो कुछ... तकनीकी दिक्कतें मुझे ब्लागियाने के दौरान झेलनी पडती हैं उन पर भी चर्चा हुई.
अभी हमारी बातचीत पूरी भी नहीं हुई थी कि मीटिंग का समय हो गया और हम संस्थान से कार्यालय की ओर कूच कर गए. ढाई-तीन घंटे की बैठक के बाद सवाल उठा कि अब। राव साहब चाहते थे कि मैं उनके घर की ओर चलूँ और मुझे ट्रेन पकड़नी थी। अव्वल तो बहुत थोड़े ही समय में राव साहब से जैसी आत्मीयता हुई, कम ही लोगों से हो पाती है। जो सहज और पारिवारिक व्यवहार उनका है, वह उनके साथ-साथ कानपुर से लगाव लगाने लगता है. इसलिए जाना तो मैं चाहता था, पर रेल का टाइम हो गया था और मैं उसकी अनदेखी नहीं कर सकता था. लिहाजा चलना पड़ा. कार्यालय से संस्थान तक फिर भी हम लोग साथ-साथ आए और वहाँ थोड़ी देर तक ठहरे भी. इसके बाद पौने नौ होते ही मैं स्टेशन की ओर चल पड़ा. ठीक सवा नौ बजे मैं वहाँ पहुंच भी गया.
असली त्रासदी यहीं से शुरू हुई. रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद. मालूम हुआ कि जिस रेल से मुझे जाना है वह दो घंटे विलंब से आ रही है.थोड़ी देर तक इधर-उधर टहलने के बाद मैं वेटिंग रूम में चला गया और वहीं एक खाली पडी कुर्सी पर कब्जा जमा कर नरेन्द्र मोहन जी की नई आई किताब 'संस्कृति और राष्ट्रवाद' पढने लगा. मैं पढने में मगन हो गया तो फिर रेल और समय की फिक्र भी जाती रही. हाँ कान ट्रेनों के आवागमन संबंधी घोषणाओं पर जरूर लगे हुए थे. करीब एक घंटे यानी ११ बजे तक मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं थी. ११ बजे यह घोषणा हुई कि गाडी संख्या ४१५ अपने निर्धारित समय से पौने तीन घंटे देर है. तो भी मैंने कहा कोई बात नहीं. अब १२ बजे तक आराम से पढेंगे. इसके बाद ही उठेंगे. मैं पढने में लगा रहा. १२ बजे फिर घोषणा हुई कि यह ट्रेन अब चार घंटे विलंब से आ रही है. लेकिन साहब चार घंटे विलंब होने यानी रात के डेढ़ बजने तक जब ट्रेन नंबर ४१५ के संबंध में कोई और घोषणा नहीं हुई तो मुझे लगा कि यह क्या ट्रेन नंबर ४२० हो गई.
आख़िर मैं वहाँ से उठा और इन्क्वायरी काउंटर गया. वहाँ मालूम हुआ साहब अभी कोई सूचना नहीं है, हाँ आएगी वह प्लेटफार्म नंबर दो पर ही. मैंने सोचा जब कोई सूचना नहीं है तो क्या भरोसा, अचानक आ ही जाए? बेहतर यही है कि प्लेटफार्म नंबर दो पर ही चला जाए. वहाँ हमारे जैसे सैकड़ों रेलपीडित अतृप्त आत्माओं की तरह इधर-उधर भटक रहे थे. सबका दर्द यही था कि रेल को दो-चार-छः नहीं चौबीस घंटे देर से भी आना हो तो कोई बात नहीं, पर हाकिमान यह बता तो दें कि कितनी देर लगेगी.
इस गलतबयानी का नतीजा यह होता है कि तमाम यात्री आ कर स्टेशन पर अनायास टपकते रहते हैं. न तो उनका कोई पुरसाहाल होता है और न कोई उद्देश्य ही हल होता है. इंतज़ार की इस लें में ऐसे मरीज भी हो सकते हैं जिनके लिए इधर-उधर भटकना नुकसानदेह हो सकता है. यूँ तो यह स्वस्थ आदमी के लिए भी नुकसानदेह है. और यात्रियों की छोड़िये, यह तो रेल के लिए भी नुकसानदेह है. इसे गलतबयानी या सही आकलन की क्षमता का अभाव, जो भी कह लें, का ही नतीजा है जो प्लेट्फार्मों पर अनावश्यक भीड़ हमेशा दिखाई देती है. ठीक समय मालूम न होने के नाते यात्रियों को वहाँ भटकना पड़ता है. और कई यात्रियों के साथ उन्हें पहुँचाने आए लोगों को भी भटकना पङता है. बेमतलब ही भीड़ बढती जाती है और शोर बढ़ता जाता है.
इस भीड़ का फायदा अराजक तत्त्व उठाते हैं. ऎसी ही स्थितियों में कभी कहीँ विस्फोट होता है तो कहीँ भगदड़ मचाती है और इस सबमें सैकड़ों लोगों की जानें जाती हैं. रेल कुछ न करे, केवल समय से सही सूचनाओं की लेन-देन का इंतजाम भर बना ले तो न केवल रेल, बल्कि यात्रियों और देश की भी आधी समस्यायें हल हो जाएंगी. बहरहाल साहब, अपने राम वहाँ घूमते रहे. चूंकि ठसाठस भरे प्लेटफार्म पर बैठाने के लिए कोई जगह थी नहीं, लिहाजा पढाई भी नहीं की जा सकती थी. मजबूरन इधर-उधर घूमते रहे. रात के साढ़े तीन बज गए. इस बीच कई दूसरी ट्रेनें उसी प्लेटफार्म से आईं-गईं. पर ४१५ के बारे में कोई घोषणा तक नहीं हुई.
घोषणा हुई साढ़े तीन बजे और वह भी सिर्फ इतनी कि अब वह प्लेटफार्म नंबर २ नहीं १ पर आएगी. इस पर जो कुछ लोग परिवार समेट आकर दो नंबर प्लेटफार्म पर बैठ चुके थे और जिनके साथ ज्यादा सामान भी थे उन्होने रेल के अफसरों-कर्मचारियों से अपने निकट संबंधों के दावे शुरू कर दिए. काश बिना किसी माइक के की जाने वाली यात्रियों की ये प्रीतिकर घोषणाएँ रेल की व्यवस्था के कान तक पहुंच पाते. आखिरकार वह चिर-प्रतीक्षित शुभ मुहूर्त आ ही गया जब रेल आ गयी. भोर के चार बजे. सारे यात्रियों के साथ मैं भी भागा और जैसे-तैसे अपना डिब्बा तलाश कर उसमें लदा. लद कर व्यवस्थित होते ही एक यात्री ने अपने साथी से सवाल किया जब देर से आयी है तो पहुँचेगी भी देर ही से? 'अरे आ गयी यही क्या कम है, जो अब पहुँचाने की भी सोचने लगे? देर की बात छोड़ दो. पहुंच जाओ बस यही मनाओ. यूँ तो रेल में तब तक बैठो ही नहीं जब तक फुरसतिए न हो. भारतीय रेल फुरसतियों की ही है.' जबकि मैं
इष्ट देव सांकृत्यायन




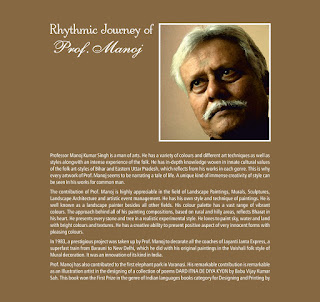


सत्य!! भारतीय रेल का एक बुरा अनुभव हम झेल चुके हैं।
ReplyDeleteसुन रहै हो ना ज्ञान दद्दा, ई देखौ ईयत्ता वाले भैय्या माननीय मंत्री जी के लिए का कह रहै हैं भला!!
ये ल्लो। असली नारद नकली नारद की तर्ज पर फुरसतिया भी असली नकली होने लगे। बहुत सही। देखिये हमसे आपकी मुलाकात का असर कि मिलते ही आपकी पोस्ट की लम्बाई बढ़ गयी। है कि नहीं !
ReplyDeleteआप भी खूब फुरसत से लिखे हैं, लगता है कि स्टेशन पर बैठे-हांडते ही ड्राफ्ट बना लिया था :)
ReplyDeleteइस प्रकरण पर ज्ञानदत्तजी से कोई सफाई मांगना कोई समझदारी का काम नहीं है- है क्या ?
और हॉं- देश को गांवशून्य बनाने के प्रति हमारी कतई सहमति नहीं है- अतानु की है, श्री की नहीं है- हम तो इन 'दो बांको' के तेवर पर मुंडी हिला रहे थे।
मसिजीवी भाई
ReplyDeleteअरे जब टेसन लगातार आठ घंटा मनई टेंसन झेलेगा तो डराफ्ट तो बनिए जाएगा. हाँ ई जान के अच्छा जरूर लगा कि आप देश को गांवशून्य बनाने के पक्ष में नहीं हैं. असल में आपकी मूडी हमको अतानु की ओर हिलती दिख रही थी. हमको भरम हो गया होगा.
आपकी भाषा बहुत पठनीय एवं आनंददायक है. लेख उपयोगी है, भाषा पढने लायक
ReplyDeleteभगवान का शुक्र है कि इष्टदेव सांक़ृत्यायन जी से मेरा परिचय नहीं है! अच्छा है केवल माननीय मंत्री महोदय को लपेटा जा रहा है.
ReplyDeleteप्रतिष्ठार्थ
ReplyDeleteश्री ज्ञानदत्त पाण्डेय
इस मुगालते में मत रहिए पाण्डेय जी, हम आपको अक्सर पढ़ते रहते हैं. तो परिचय तो हइये है, खाली ताका झांकी नहीं है. उहो हो जाएगा किसी दिन. फिर का करिएगा? अरे सुधर पाइये तो हई तो रेलिया आप दौडा रहे हैं, इसको सुधारिये.
आपने अपना रेल उत्पीड़्न का अनुभव सुनाया, पसंद आया। आपने सही कहा कि रेल को गॉड चलाता है।
ReplyDelete