मीडिया का संकट
पत्रकारिता पर इधर ख़ूब लिखा जा रहा है. अविनाश भाई की सदारत वाला मोहल्ला इन दिनों मीडिया को ही लेकर हल्ले का केंद्र बन गया है. इस हल्ले की शुरुआत वैसे तो काफी पहले हो चुकी थी, पर इसे गति दीं दिलीप मंडल के एक पोस्ट ने. दिलीप ने इसमें मीडिया के अतीत का कच्चा चिटठा खोलते हुए कहना चाहा है कि आज दिखाई दे रही यह मूल्यहीनता कोई नई बात नहीं है और इसलिए युवा पत्रकारों को किसी हीनताग्रंथि का शिकार होने की जरूरत नहीं है. दूसरी बात यह कि मीडिया के इस पतितपने के पीछे कुछ मजबूरियां हैं उन्हें भी समझा जाना चाहिए. तीसरी बात यह कि मीडिया अगर इधर बिगडा है तो वह कई मायनों में बहुत कुछ सुधरा भी है और वह सुधर भी देखा जाना चाहिए. बस. मेरी समझ से उनका मंतव्य यहीं तक था. इसके बाद मोहल्ले में बहुत लोगों ने बहुत कुछ प्रतिक्रियाएँ कीं. मामला मोहल्ले से कस्बे तक पहुंच गया. आखिरकार टाउन एरिया चेयरमैन रवीश भाई को बोलना पड़ा. उनहोंने नए दौर को हिंदी पत्रकारिता का प्रश्न काल कहा और बताया कि मीडिया आज अपनी आलोचना के संदर्भ में जितनी अंतर्मुखी है उतनी कभी नहीं थी. यह बात सौ फीसदी सच है.
एक ऐसे दौर में जबकि इस लोकतंत्र के भ्रष्ट तंत्र में कोई पाया अपने गिरेबान में झांकने के लिए तैयार नहीं है, चौथा खम्बा तब भी बार-बार अपने ही आईने में खुद को बार-बार देख रहा है. आत्मनिरीक्षण कर रहा है. यह तथ्य ही काफी है यह साबित करने के लिए कि बाकी तंत्रों की तुलना में (तुलना के नाम पर नाक-भौं सिकोड़ने वाले दर्ज कर लें कि तुलना से कुछ भी मुक्त नहीं है. यहाँ तक कि दार्शनिक सिद्धांतों की प्रासंगिकता आंकने के लिए भी कई समकालीन सिद्धांतों को एक तल पर रखा जाता है) यह आज भी बहुत नैतिक और मूल्यकेंद्रित है. बाहर-भीतर हजार तरह से लात-जूते खाकर और कुढ़ कर भी. चूंकि हम खुद बार-बार अपने गिरेबान में झांक रहे हैं, लिहाजा यह तय है कि हम पूरी तरह पतित कभी नहीं हो सकेंगे. और एक विरोधाभासी बात यह कि लगातार बिगड़ते हुए भी लगातार सुधरते रहेंगे. रही बात भूत-प्रेत-गड्ढे और गन्ने के खेत वाली पत्रकारिता की, तो उसके दिन अब बहुत दिन शेष नहीं हैं. आज जिस बाजार के इशारे पर मीडिया नाच रही है और जिसके लिए वह यह सब टोटके कर रही है, वह बाजार ही इसे मजबूर करेगा इस खाके से बाहर आने के लिए.
यह किन बातों का नतीजा हैं, इस पर फिर कभी. लेकिन एक बात हम भूल रहे हैं और वह है पत्रकारों पर बढ़ते खतरों की. दुनिया भर की बातों में खोए हम खुद को भूल चुके हैं. हम गड्ढे में गिरे प्रिंस की बात तो करते हैं लेकिन अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान सीआरपीएफ की लाठियों से लहूलुहान हुए निखिल और संजीव टोनी की बात नहीं करते. इन्हें केवल इसलिए लिटा-लिटा कर मारा गया कि इन्होने जबरिया मुफ़्त की शराब पी कर सड़क पर ग़दर काटते सीआरपीएफ जवानों की तसवीरें खींचने की कोशिश की. पंजाब के जालंधर शहर की इस घटना में फोटोग्राफर संजीव टोनी का कैमरा भी तोड़ दिया गया और मोटरसाइकिल भी चौपट कर दी गयी. वहाँ खडी पंजाब पुलिस और उनका एक एसपी तमाशबीन बने रहे.
इन प्रेसकर्मियों को बचाने सिर्फ आम जनता आयी और जाहिर है ऐसा उसने सिर्फ इसीलिए किया कि हम कहीं न कहीं उसके विश्वासों की रक्षा करते हैं. उसके हितों से जुडे हैं. इस अच्छी कोशिश का खमियाजा जालंधर के दो आम नौजवानों को भुगतना पड़ा. एक व्यक्ति की तो आँखें ही निकाल ली गईं. सीआरपीएफ के जांबाज जवानों ने इस महान काम को युवकों का अपहरण करके उन्हें एक थाने में ले जाकर अंजाम दिया. यानी पुलिस लगातार मूक दर्शक बनी रही और सीआरपीएफ अपनी ड्यूटी (?) बजाती रही.
मुझे हैरत हुई यह देखकर कि हमारी दिल्ली की मीडिया (केवल टीवी चैनल ही नहीं अखबारों तक) ने इस घटना को कोई खास तवज्जो नहीं दीं. अरे भाई कभी-कभी तो टीआरपी और सर्कुलेशन के प्रेत प्रभाव से मुक्त हो जाओ. और फिर यह मसला तो आम जनता से भी जुड़ा है. सवाल यह है कि अगर हम खुद अपने प्रति ही जिम्मेदार साबित न हो सके तो किसी और के प्रति हमारी जिम्मेदारी का मतलब ही क्या बचेगा? क्या आप यह उम्मीद करते हैं कि यह जिम्मेदारी कोई और निभाएगा? बताइए कौन से खंभे से उम्मीद है आपको?
यह घटना यह स्पष्ट करने के लिए काफी है कि पत्रकारिता आज भी तलवार की धर पर नंगे पैर चलने जैसा ही पेशा है. इस नट्गीरी का जो मेहनताना मिलता है वह भी किसी से छिपा नहीं है. यह तो आप सब जानते ही होंगे कि पूरे देश में पत्रकारों की स्थिति (आर्थिक मामलों में) दिल्ली - मुम्बई के टीवी चैनलों के सीनियर प्रोड्यूसरों जैसी नहीं है. यह आपके गर्व से फूल कर कुप्पा हो जाने वाली बात नहीं है. अपनी दुनिया की जमीनी सच्चाई से अगर आज आप वाकिफ न भी हों तो कल हो जाएंगे. इसलिए अब यह सोचना जरूरी हो गया है कि इन हालत में सच्ची कैसे जिंदा रहेगी? परिवार-अख़बार-सरकार-बाजार के चौतरफा दबावों के बीच पिस्ता एक पत्रकार सच कहने की जोखिम कितने दिन मोल ले सकेगा? क्या यह सोचना हमारा कर्तव्य नहीं है और क्या यह भी आत्मनिरीक्षण का एक सार्थक प्रयास नहीं होगा?
इष्ट देव सांकृत्यायन
एक ऐसे दौर में जबकि इस लोकतंत्र के भ्रष्ट तंत्र में कोई पाया अपने गिरेबान में झांकने के लिए तैयार नहीं है, चौथा खम्बा तब भी बार-बार अपने ही आईने में खुद को बार-बार देख रहा है. आत्मनिरीक्षण कर रहा है. यह तथ्य ही काफी है यह साबित करने के लिए कि बाकी तंत्रों की तुलना में (तुलना के नाम पर नाक-भौं सिकोड़ने वाले दर्ज कर लें कि तुलना से कुछ भी मुक्त नहीं है. यहाँ तक कि दार्शनिक सिद्धांतों की प्रासंगिकता आंकने के लिए भी कई समकालीन सिद्धांतों को एक तल पर रखा जाता है) यह आज भी बहुत नैतिक और मूल्यकेंद्रित है. बाहर-भीतर हजार तरह से लात-जूते खाकर और कुढ़ कर भी. चूंकि हम खुद बार-बार अपने गिरेबान में झांक रहे हैं, लिहाजा यह तय है कि हम पूरी तरह पतित कभी नहीं हो सकेंगे. और एक विरोधाभासी बात यह कि लगातार बिगड़ते हुए भी लगातार सुधरते रहेंगे. रही बात भूत-प्रेत-गड्ढे और गन्ने के खेत वाली पत्रकारिता की, तो उसके दिन अब बहुत दिन शेष नहीं हैं. आज जिस बाजार के इशारे पर मीडिया नाच रही है और जिसके लिए वह यह सब टोटके कर रही है, वह बाजार ही इसे मजबूर करेगा इस खाके से बाहर आने के लिए.
यह किन बातों का नतीजा हैं, इस पर फिर कभी. लेकिन एक बात हम भूल रहे हैं और वह है पत्रकारों पर बढ़ते खतरों की. दुनिया भर की बातों में खोए हम खुद को भूल चुके हैं. हम गड्ढे में गिरे प्रिंस की बात तो करते हैं लेकिन अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान सीआरपीएफ की लाठियों से लहूलुहान हुए निखिल और संजीव टोनी की बात नहीं करते. इन्हें केवल इसलिए लिटा-लिटा कर मारा गया कि इन्होने जबरिया मुफ़्त की शराब पी कर सड़क पर ग़दर काटते सीआरपीएफ जवानों की तसवीरें खींचने की कोशिश की. पंजाब के जालंधर शहर की इस घटना में फोटोग्राफर संजीव टोनी का कैमरा भी तोड़ दिया गया और मोटरसाइकिल भी चौपट कर दी गयी. वहाँ खडी पंजाब पुलिस और उनका एक एसपी तमाशबीन बने रहे.
इन प्रेसकर्मियों को बचाने सिर्फ आम जनता आयी और जाहिर है ऐसा उसने सिर्फ इसीलिए किया कि हम कहीं न कहीं उसके विश्वासों की रक्षा करते हैं. उसके हितों से जुडे हैं. इस अच्छी कोशिश का खमियाजा जालंधर के दो आम नौजवानों को भुगतना पड़ा. एक व्यक्ति की तो आँखें ही निकाल ली गईं. सीआरपीएफ के जांबाज जवानों ने इस महान काम को युवकों का अपहरण करके उन्हें एक थाने में ले जाकर अंजाम दिया. यानी पुलिस लगातार मूक दर्शक बनी रही और सीआरपीएफ अपनी ड्यूटी (?) बजाती रही.
मुझे हैरत हुई यह देखकर कि हमारी दिल्ली की मीडिया (केवल टीवी चैनल ही नहीं अखबारों तक) ने इस घटना को कोई खास तवज्जो नहीं दीं. अरे भाई कभी-कभी तो टीआरपी और सर्कुलेशन के प्रेत प्रभाव से मुक्त हो जाओ. और फिर यह मसला तो आम जनता से भी जुड़ा है. सवाल यह है कि अगर हम खुद अपने प्रति ही जिम्मेदार साबित न हो सके तो किसी और के प्रति हमारी जिम्मेदारी का मतलब ही क्या बचेगा? क्या आप यह उम्मीद करते हैं कि यह जिम्मेदारी कोई और निभाएगा? बताइए कौन से खंभे से उम्मीद है आपको?
यह घटना यह स्पष्ट करने के लिए काफी है कि पत्रकारिता आज भी तलवार की धर पर नंगे पैर चलने जैसा ही पेशा है. इस नट्गीरी का जो मेहनताना मिलता है वह भी किसी से छिपा नहीं है. यह तो आप सब जानते ही होंगे कि पूरे देश में पत्रकारों की स्थिति (आर्थिक मामलों में) दिल्ली - मुम्बई के टीवी चैनलों के सीनियर प्रोड्यूसरों जैसी नहीं है. यह आपके गर्व से फूल कर कुप्पा हो जाने वाली बात नहीं है. अपनी दुनिया की जमीनी सच्चाई से अगर आज आप वाकिफ न भी हों तो कल हो जाएंगे. इसलिए अब यह सोचना जरूरी हो गया है कि इन हालत में सच्ची कैसे जिंदा रहेगी? परिवार-अख़बार-सरकार-बाजार के चौतरफा दबावों के बीच पिस्ता एक पत्रकार सच कहने की जोखिम कितने दिन मोल ले सकेगा? क्या यह सोचना हमारा कर्तव्य नहीं है और क्या यह भी आत्मनिरीक्षण का एक सार्थक प्रयास नहीं होगा?
इष्ट देव सांकृत्यायन




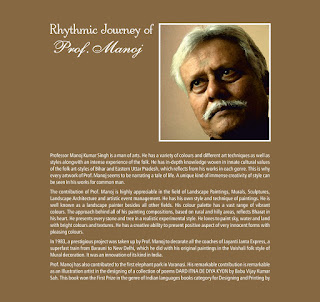


अच्छा लिखा है।
ReplyDeleteबिल्कुल सही कहा गया. आभार.
ReplyDeleteमेरी पोस्ट खबर क्या है, पढ़िये, आपको कुछ जवाब मिल जाएंगे. क्या हुआ जवाब मिला या नहीं.
ReplyDeleteइष्ट देव उवाच> ...इस नट्गीरी का जो मेहनताना मिलता है वह भी किसी से छिपा नहीं है. यह तो आप सब जानते ही होंगे कि पूरे देश में पत्रकारों की स्थिति (आर्थिक मामलों में) दिल्ली - मुम्बई के टीवी चैनलों के सीनियर प्रोड्यूसरों जैसी नहीं है.
ReplyDeleteहमारा सोचना था कि पत्रकार लोग कुबेर के कुनबे के भले न हों; पर आर्थिक रूप से इतने असुरक्षित भी नहीं हैं. ये बतायें कि यह असुरक्षा चादर के अन्दर रहने पर भी है? और यह ईमानदार सवाल है - कोई व्यंग नहीं है इसमें.
सही लिखा।
ReplyDeleteक्या पत्रकार की यह नियति हो गई है कि जब भी वह वर्दीधारी गुंडों, खद्दरधारी लुच्चों को आइना दिखने की कोशिश करेगा लाठियाँ,घूँसे, गालियाँ खायेगा... आख़िर क्यूं और कब तक? खासतौर पर कस्बाई पत्रकार जिस पीडा को भोगते हैं उसकी आंच शायद ही कभी राजधानी में बैठे सजातिए बंधुओं ने महसूस की हो !! शायद इसीलिये हमारी दिल्ली की मीडिया ने इस घटना को कोई खास तवज्जो नहीं दीं...
ReplyDeleteआपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं इष्टदेव जीं... अब यह सोचना निहायत जरूरी हो गया है कि इन हालत में सच्ची कैसे जिंदा रहेगी? परिवार-अख़बार-सरकार-बाजार के चौतरफा दबावों के बीच पिसता एक पत्रकार सच कहने की जोखिम कितने दिन मोल ले सकेगा? इन पर खुलकर चर्चा होनी ही चाहिऐ .होगी आज नहीं तो कल ... करनी ही होगी यदि पत्रकारिता को जिंदा रखना है तो... सच्च को जिंदा रखनाहै तो ...
बहुत अच्छा कहा है गुरू
ReplyDeleteसत्येंद्र
गोरखपुर
सही!!
ReplyDeleteज्ञान दद्दा, रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी हैं यहां कई अखबार ऐसे हैं जहां तीन महीने मे एक बार तनख्वाह मिलती हैं जबकि उसके मालिक लाखों रुपए हर महीने कमाते हैं ऐसा नही है कि यह अखबार छुटभैय्ये टाइप ही हैं कुछ नामी अखबार( मालिक तो और भी नामी हैं) की भी यही हालत है!