क्यों नहीं समझते इतनी सी बात?
लालगढ़ में माओवादियों को घेरने का क़रीब-क़रीब पूरा इंतज़ाम कर लिया गया है. मुमकिन है कि जल्दी ही उनसे निपट लिया जाए और फिलहाल वहां यह समस्या हल कर लिए गए होने की ख़बर भी आ जाए. लेकिन क्या केवल इतने से ही यह समस्या हल हो जाएगी? लालगढ़ में माओवादियों ने प्रशासन और सुरक्षाबलों को छकाने का जो तरीक़ा चुना है, वह ख़ास तौर से ग़ौर किए जाने लायक है. यह मसला मुझे इस दृष्टि से बिलकुल महत्वपूर्ण नहीं लगता कि माओवादी क्या चाहते हैं या उनकी क्या रणनीति है. लेकिन यह इस दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है कि माओवादी जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने यह जो रणनीति बनाई है वह सफल कैसे हो जा रही है. क्या उसका सफल होना केवल एक घटना है या फिर हमारी कमज़ोरी या फिर हमारी सामाजिक विसंगतियों का नतीजा या कि हमारी पूरी की पूरी संसदीय व्यवस्था की विफलता? या फिर इन सबका मिला-जुला परिणाम?
यह ग़ौर करने की ज़रूरत है कि माओवादी विद्रोहियों ने अपने लिए लालगढ़ में जो सुरक्षा घेरा बना रखा था उसमें सबसे आगे महिलाएं थीं और बच्चे थे. महिलाओं और बच्चों के मामले में केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरे भारत का नज़रिया एक सा है. उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक. केवल उनके प्रति संवेदनशीलता और उनकी हिफ़ाज़त के मामले में ही नहीं, उनके प्रति हैवानियत के मामले में भी. कोई आसानी से अपने परिवार की महिलाओं, बच्चों या बुजुर्गों को कहीं भिड़ने नहीं भेजता. पर माओवादियों को बचाने के लिए वे यह भी करने को तैयार हो गए तो क्यों? अब यह एक अलग बात है कि माओवादी और नक्सली एक ही बात नहीं है, पर आम तौर पर इन्हें एक ही समझा जाता है. ख़ैर समझने का क्या करिएगा! समझने का तो आलम यह है कि मार्क्सवाद और माओवाद का फ़र्क़ भी बहुत लोग नहीं जानते, पर इससे मार्क्सवाद माओवाद नहीं हो जाता और न अगली पंक्ति के सभी मार्क्सवादियों के व्यवहार में धुर माओवादी या फासीवादी हो जाने से ही ऐसा हो जाता है. बहरहाल, समाज का शोषित-वंचित तबका जब इन्हें बचाने के लिए अपने और अपने प्रियजनों के प्राणों की बाजी तक लगाने के लिए तैयार हो जाता है तो उसके मूल में किसी मार्क्सवाद, माओवाद, स्टालिनवाद या नक्सलवाद का कोई खांचा नहीं होता है. दुनिया के किसी सिद्धांत से उसका कोई मतलब नहीं होता है.
फिर भी यह देखा जाता है कि वह अपना सब कुछ इनके लिए लुटाने को तैयार हो जाता है. यह बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है. नक्सली झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छ्त्तीसगढ़, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में भी फैले हैं. सरकारी और पूंजीवादी मीडियातंत्र द्वारा दुष्प्रचार के तमाम टोटके अपनाए जाने के बावजूद इन्हें वहां की आम जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है. सिर्फ़ इन्हें ही नहीं, इनके जैसे कई दूसरे संगठनों-गिरोहों को भी जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है. भारतीय समाज में बहुत जगहों पर डकैत भी ऐसे ही अपना अस्तित्व बनाए रखने में सफल साबित होते रहे हैं, बावजूद इसके कि उनका ऐसा कोई वाद-सिद्धांत नहीं होता रहा है और न वे किसी बड़े-व्यापक परिवर्तन का सपना ही दिखाते रहे हैं. और हां, इसका मतलब यह भी न निकालें कि मैं डाकुओं, नक्सलियों और माओवादियों को एक समान मान रहा हूं. बुनियादी बात बस यह है कि जनसमर्थन उन्हें भी हासिल होता रहा है. और ऐसा केवल हमारे देश में होता हो, यह भी नहीं है. दुनिया का इतिहास पलट कर देखें तो ऐसे हज़ारों उदाहरण दूसरे देशों में भी मिल जाएंगे. इस तरह देखें तो हमारे समाज में जनसमर्थन हासिल करने का मतलब किसी दर्शन या सिद्धांत के प्रति लोगों का समर्थन या उनकी आस्था हासिल करना नहीं होता है. जब बहुत सारे लोग अपनी और अपने बाल-बच्चों की जान की परवाह छोड़ कर नक्सलियों-माओवादियों का साथ दे रहे होते हैं तो उनके मन में कुछ बहुत गहरे असंतोष होते हैं, रोष होते हैं. उनकी कुछ ज़रूरतें हैं, जिनको वे किसी न किसी तरह एक नियत हद तक शायद पूरी कर देते हैं. यह ग़ौर करने की बात है कि समाज का एक ही ख़ास तबका है जिसे अधिकतर नक्सली या माओवादी संगठन अपना निशाना बनाते हैं. नेपाल से लेकर चेन्नई तक फैले जंगलों में वे इसी ख़ास तबके को लेकर बढ़ते चले गए हैं. बावजूद इसके कि दोनों की हालत अभी तक जस की तस है, ये हक़ीक़त है कि पुलिस के लिए वनवासियों या ग्रामीणों से उनके बारे में किसी तरह का सुराग पाना आसान बात नहीं है. क्यों? क्योंकि आम जनता पुलिस पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं करती, लेकिन नक्सलियों और माओवादियों पर पूरा भरोसा करती है. यहां तक कि डाकुओं और आतंकवादियों पर भी भरोसा कर लेती है, पर पुलिस पर वह भरोसा नहीं करती.
ख़ैर भरोसे पर बात बाद में. बुनियादी बात यह है कि उस एक ख़ास तबके को ही पकड़ कर ये आगे फैलते क्यों जाते हैं? क्योंकि यह हमारे समाज का वह तबका है जो बेहद शोषित और पूरी तरह वंचित है. विकास के नए उपादानों का तो उसे कोई लाभ नहीं ही मिल सका है, उसकी रही-सही ज़मीन भी उसके पैरों तले से छीन ली जा रही है. उनके संसाधनों की इस लूट को व्यवस्था की खुली छूट है.
इसका एहसास लूटने वाले हमारे तंत्र को हो न हो, पर भुगतने वालों को तो दर्द टीसता ही है. इसी टीस की पहचान उन्हें है. इसका लाभ वे उठा रहे हैं. और यक़ीनन, वे उसका सिर्फ़ लाभ ही उठा रहे हैं. बिलकुल वैसे ही जैसे हमारा पूंजीवादी तंत्र वनवासियों के भोलेपन और संसाधनों का लाभ उठा रहा है. पर वनवासियों की मजबूरी यह है कि उन्हें इस तथाकथित सभ्य व्यवस्था के पेंचो-खम पता नहीं हैं. इसलिए वे इसके कई पाटों के बीच पिस कर रह जाते हैं. जब नक्सली आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि उनके हक़ की लड़ाई वे लड़ेंगे, तो उनका सहज ही विश्वास कर लेना बहुत ही साधारण बात है. बिलकुल ऐसे ही ग्रामीण डाकुओं की बातों पर भरोसा कर लेते थे. कहीं-कहीं आज भी कर लेते हैं और आगे भी करते रहेंगे. यही बात है जो लालगढ़ में लोगों को माओवादियों की सुरक्षा के लिए आगे खड़े हो जाने के लिए विवश कर रही है.
हालांकि, ख़ास लालगढ़ के सन्दर्भ में यह मामला कई और मसलों पर सोचने के लिए विवश करता है. पर उन सब पर फिर कभी. अभी तो सिर्फ़ इस सवाल का जवाब मैं चाहता हूं कि मान लें लालगढ़ की हालिया समस्या हल कर लेंगे. मान लेते हैं कि वहां सारे माओवादियों को मार गिराएंगे. तो भी क्या इतने से यह समस्या हल हो जाएगी? क्या इसके बाद फिर माओवादी कहीं अपने पैर पसार नहीं सकेंगे? यह क्यों भूलते हैं कि जो लोग उनके प्रति सहानुभूति रखने वाले हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है. अब सिर्फ़ वनवासी ही नहीं, ग्रामीण किसान भी धीरे-धीरे उसी स्थिति में पहुंच रहे हैं जिस स्थिति में पिछली कई शताब्दियों से वनवासी हैं. गांव का किसान अपने को पूरी तरह लुटा-पिटा महसूस कर रहा है. व्यवस्था उसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ उपेक्षा ही कर रही है. पिछले 20 सालों में देश में केंद्र या किसी राज्य की भी सरकार ने किसानों के हित में कोई नीति बनाई हो, ऐसा मुझे याद नहीं आता. ग़ौर से देखें तो शहरों में एक ऐसा ही तबका है, जो शेष आबादी से कटा हुआ है. शहर की ज़िन्दगी की जो मुख्यधारा कही जाती है उसके हाशिए से भी वह बाहर है. ये सभी जो वर्ग हैं, इन्हें पहले व्यवस्था ने शिकार बनाया है इनके भीतर की मलाई निकालने के लिए और आने वाले दिनों में माओवादी या ऐसे ही दूसरे संगठन इन्हें अपना शिकार बनाएंगे. इनका उपयोग कर व्यवस्था की मलाई हासिल करने के लिए.
वह स्रोत जिससे ऐसे संगठनों को ऊर्जा मिलती है आगे बढने की वह कोई मनुष्य नहीं, बल्कि आम आदमी के भीतर मौजूद भूख है. यह भूख सिर्फ़ पेट की नहीं है, यह भूख सामान्य मानवीय भावनाओं की भी है. आत्मसम्मान और स्वाभिमान की भी है. मनुष्य के सचमुच का मनुष्य बन कर जीने की भूख है. इसके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ़ इतना ही तो करना है कि व्यवस्था के शीर्ष पर जो लोग मौजूद हैं, उन्हें अपनी हबस थोड़ी कम कर देनी है. क्या यह बहुत मुश्किल बात है? अगर नहीं तो फिर सिर्फ़ इतना क्यों नहीं कर देते वे? या फिर उन्हें यह बात समझ में नहीं आती कि कल इसका नतीजा क्या निकलेगा?
यह ग़ौर करने की ज़रूरत है कि माओवादी विद्रोहियों ने अपने लिए लालगढ़ में जो सुरक्षा घेरा बना रखा था उसमें सबसे आगे महिलाएं थीं और बच्चे थे. महिलाओं और बच्चों के मामले में केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरे भारत का नज़रिया एक सा है. उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक. केवल उनके प्रति संवेदनशीलता और उनकी हिफ़ाज़त के मामले में ही नहीं, उनके प्रति हैवानियत के मामले में भी. कोई आसानी से अपने परिवार की महिलाओं, बच्चों या बुजुर्गों को कहीं भिड़ने नहीं भेजता. पर माओवादियों को बचाने के लिए वे यह भी करने को तैयार हो गए तो क्यों? अब यह एक अलग बात है कि माओवादी और नक्सली एक ही बात नहीं है, पर आम तौर पर इन्हें एक ही समझा जाता है. ख़ैर समझने का क्या करिएगा! समझने का तो आलम यह है कि मार्क्सवाद और माओवाद का फ़र्क़ भी बहुत लोग नहीं जानते, पर इससे मार्क्सवाद माओवाद नहीं हो जाता और न अगली पंक्ति के सभी मार्क्सवादियों के व्यवहार में धुर माओवादी या फासीवादी हो जाने से ही ऐसा हो जाता है. बहरहाल, समाज का शोषित-वंचित तबका जब इन्हें बचाने के लिए अपने और अपने प्रियजनों के प्राणों की बाजी तक लगाने के लिए तैयार हो जाता है तो उसके मूल में किसी मार्क्सवाद, माओवाद, स्टालिनवाद या नक्सलवाद का कोई खांचा नहीं होता है. दुनिया के किसी सिद्धांत से उसका कोई मतलब नहीं होता है.
फिर भी यह देखा जाता है कि वह अपना सब कुछ इनके लिए लुटाने को तैयार हो जाता है. यह बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है. नक्सली झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छ्त्तीसगढ़, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में भी फैले हैं. सरकारी और पूंजीवादी मीडियातंत्र द्वारा दुष्प्रचार के तमाम टोटके अपनाए जाने के बावजूद इन्हें वहां की आम जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है. सिर्फ़ इन्हें ही नहीं, इनके जैसे कई दूसरे संगठनों-गिरोहों को भी जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है. भारतीय समाज में बहुत जगहों पर डकैत भी ऐसे ही अपना अस्तित्व बनाए रखने में सफल साबित होते रहे हैं, बावजूद इसके कि उनका ऐसा कोई वाद-सिद्धांत नहीं होता रहा है और न वे किसी बड़े-व्यापक परिवर्तन का सपना ही दिखाते रहे हैं. और हां, इसका मतलब यह भी न निकालें कि मैं डाकुओं, नक्सलियों और माओवादियों को एक समान मान रहा हूं. बुनियादी बात बस यह है कि जनसमर्थन उन्हें भी हासिल होता रहा है. और ऐसा केवल हमारे देश में होता हो, यह भी नहीं है. दुनिया का इतिहास पलट कर देखें तो ऐसे हज़ारों उदाहरण दूसरे देशों में भी मिल जाएंगे. इस तरह देखें तो हमारे समाज में जनसमर्थन हासिल करने का मतलब किसी दर्शन या सिद्धांत के प्रति लोगों का समर्थन या उनकी आस्था हासिल करना नहीं होता है. जब बहुत सारे लोग अपनी और अपने बाल-बच्चों की जान की परवाह छोड़ कर नक्सलियों-माओवादियों का साथ दे रहे होते हैं तो उनके मन में कुछ बहुत गहरे असंतोष होते हैं, रोष होते हैं. उनकी कुछ ज़रूरतें हैं, जिनको वे किसी न किसी तरह एक नियत हद तक शायद पूरी कर देते हैं. यह ग़ौर करने की बात है कि समाज का एक ही ख़ास तबका है जिसे अधिकतर नक्सली या माओवादी संगठन अपना निशाना बनाते हैं. नेपाल से लेकर चेन्नई तक फैले जंगलों में वे इसी ख़ास तबके को लेकर बढ़ते चले गए हैं. बावजूद इसके कि दोनों की हालत अभी तक जस की तस है, ये हक़ीक़त है कि पुलिस के लिए वनवासियों या ग्रामीणों से उनके बारे में किसी तरह का सुराग पाना आसान बात नहीं है. क्यों? क्योंकि आम जनता पुलिस पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं करती, लेकिन नक्सलियों और माओवादियों पर पूरा भरोसा करती है. यहां तक कि डाकुओं और आतंकवादियों पर भी भरोसा कर लेती है, पर पुलिस पर वह भरोसा नहीं करती.
ख़ैर भरोसे पर बात बाद में. बुनियादी बात यह है कि उस एक ख़ास तबके को ही पकड़ कर ये आगे फैलते क्यों जाते हैं? क्योंकि यह हमारे समाज का वह तबका है जो बेहद शोषित और पूरी तरह वंचित है. विकास के नए उपादानों का तो उसे कोई लाभ नहीं ही मिल सका है, उसकी रही-सही ज़मीन भी उसके पैरों तले से छीन ली जा रही है. उनके संसाधनों की इस लूट को व्यवस्था की खुली छूट है.
इसका एहसास लूटने वाले हमारे तंत्र को हो न हो, पर भुगतने वालों को तो दर्द टीसता ही है. इसी टीस की पहचान उन्हें है. इसका लाभ वे उठा रहे हैं. और यक़ीनन, वे उसका सिर्फ़ लाभ ही उठा रहे हैं. बिलकुल वैसे ही जैसे हमारा पूंजीवादी तंत्र वनवासियों के भोलेपन और संसाधनों का लाभ उठा रहा है. पर वनवासियों की मजबूरी यह है कि उन्हें इस तथाकथित सभ्य व्यवस्था के पेंचो-खम पता नहीं हैं. इसलिए वे इसके कई पाटों के बीच पिस कर रह जाते हैं. जब नक्सली आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि उनके हक़ की लड़ाई वे लड़ेंगे, तो उनका सहज ही विश्वास कर लेना बहुत ही साधारण बात है. बिलकुल ऐसे ही ग्रामीण डाकुओं की बातों पर भरोसा कर लेते थे. कहीं-कहीं आज भी कर लेते हैं और आगे भी करते रहेंगे. यही बात है जो लालगढ़ में लोगों को माओवादियों की सुरक्षा के लिए आगे खड़े हो जाने के लिए विवश कर रही है.
हालांकि, ख़ास लालगढ़ के सन्दर्भ में यह मामला कई और मसलों पर सोचने के लिए विवश करता है. पर उन सब पर फिर कभी. अभी तो सिर्फ़ इस सवाल का जवाब मैं चाहता हूं कि मान लें लालगढ़ की हालिया समस्या हल कर लेंगे. मान लेते हैं कि वहां सारे माओवादियों को मार गिराएंगे. तो भी क्या इतने से यह समस्या हल हो जाएगी? क्या इसके बाद फिर माओवादी कहीं अपने पैर पसार नहीं सकेंगे? यह क्यों भूलते हैं कि जो लोग उनके प्रति सहानुभूति रखने वाले हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है. अब सिर्फ़ वनवासी ही नहीं, ग्रामीण किसान भी धीरे-धीरे उसी स्थिति में पहुंच रहे हैं जिस स्थिति में पिछली कई शताब्दियों से वनवासी हैं. गांव का किसान अपने को पूरी तरह लुटा-पिटा महसूस कर रहा है. व्यवस्था उसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ उपेक्षा ही कर रही है. पिछले 20 सालों में देश में केंद्र या किसी राज्य की भी सरकार ने किसानों के हित में कोई नीति बनाई हो, ऐसा मुझे याद नहीं आता. ग़ौर से देखें तो शहरों में एक ऐसा ही तबका है, जो शेष आबादी से कटा हुआ है. शहर की ज़िन्दगी की जो मुख्यधारा कही जाती है उसके हाशिए से भी वह बाहर है. ये सभी जो वर्ग हैं, इन्हें पहले व्यवस्था ने शिकार बनाया है इनके भीतर की मलाई निकालने के लिए और आने वाले दिनों में माओवादी या ऐसे ही दूसरे संगठन इन्हें अपना शिकार बनाएंगे. इनका उपयोग कर व्यवस्था की मलाई हासिल करने के लिए.
वह स्रोत जिससे ऐसे संगठनों को ऊर्जा मिलती है आगे बढने की वह कोई मनुष्य नहीं, बल्कि आम आदमी के भीतर मौजूद भूख है. यह भूख सिर्फ़ पेट की नहीं है, यह भूख सामान्य मानवीय भावनाओं की भी है. आत्मसम्मान और स्वाभिमान की भी है. मनुष्य के सचमुच का मनुष्य बन कर जीने की भूख है. इसके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ़ इतना ही तो करना है कि व्यवस्था के शीर्ष पर जो लोग मौजूद हैं, उन्हें अपनी हबस थोड़ी कम कर देनी है. क्या यह बहुत मुश्किल बात है? अगर नहीं तो फिर सिर्फ़ इतना क्यों नहीं कर देते वे? या फिर उन्हें यह बात समझ में नहीं आती कि कल इसका नतीजा क्या निकलेगा?




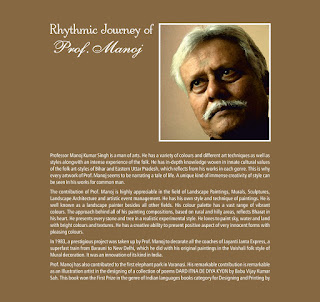


सब कुछ अर्थ की अनर्थे लीला है।
ReplyDelete@"मनुष्य के सचमुच . . . . "
सरल बातें किसे समझ में आती हैं? इसी का लाभ तो माओवादी वगैरह उठा रहे हैं।
चलिए इन्तजार करतें हैं कल का .
ReplyDeleteLalgarh jaisi ghatnaon se mukhydhara ke sarkari 'Bharat' ki 'reach' men kami ka khulasa hota hai moolbhut samasyayen agar bani hui hain,to satahi daman se kya hasil hoga...?
ReplyDeletevicharotezak chintan... mere gawan me ek kahawat hai- Jharkal muh Jhapne theek. lekin vyavastha ke shirsh par baithon ko apna chehra nahin dikhta...
ReplyDeleteअब कया कहे गरीब की जोरू सब की भाभी होती है, ओर गरीब को सब फ़ंसा कर अपना उल्लू सीधा कर रहे है, लेकिन उस गरीब की किसे फ़िक्र है? सरकार को? नकसल बाडियो को, मार्क्स वादी को? या माओअवादी को? किसी को नही हर कोई अपना झंडा उंचा करना चहाता है,
ReplyDeleteओर जब यग गरीब खुद मिल के उठे तो बात बन सकती है, वरना तो कठपुतली ही बने रहेगे.
आप ने बहुत सुंदर ढंग से खुल कर लिखा.
धन्यवाद
मुझे शिकायत है
पराया देश
छोटी छोटी बातें
नन्हे मुन्हे
Indian politics is fed on added problems.Let it be LalGarh or Naxalbari or anything else, these issues are like vitaminsto our leaders and bureaucrats.An article in right direction.
ReplyDeletehari shanker rarhi
माओवाद एक शैली है...इममें चिंतन भी शामिल है और युद्ध रणनीति भी...और इसका एकमात्र उद्देश्य है वर्तमान व्यवस्था को उखाड़ फेंकना...औरतों को अग्रमि पंक्ति में खड़ा करना माओवाद युद्ध शैली का एक हिस्सा है...और यह काफी कारगर होता है....जहां पर उनका कब्जा हो चुका है उसे वे लोग अपनी शब्दावली में लिबरेटेड लैंड कहते हैं...और एक दिन वे लोग पूरे भारत को लिबरेट करने की बात करते हैं...यानि की सबकुछ सपाट कर देंगे...विकास से वंचित इलाकों में इन्हें पैर पसारने का अच्छा मौका मिल गया है...माओ शैली में दम है इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता....दुनिया को देखने का उनका अपना नजरिया है..और वह नजरिया काफी मजबूत है...हां स्वतंत्र भारत में खून की होली खेलने की इजाजत कियी को नहीं दी जा सकती है...चाहे वो माओवादी हो या फिर सरकार.....
ReplyDeleteइस देश की पुलिस और न्याय-व्यवस्था अंगरेजों की भाषा बोलती-समझती है। जब जनता का उनसे संवाद ही नहीं तो भरोसा करने का सवाल ही कहां पैदा होता है। जनता की जुबान पर तो इन्होंने ब्रितानी ताला जड़ रखा है। नक्सलवादी, माओवादी, चरमपंथी व डकैत जनता की अपनी भाषा में उससे संवाद करते हैं, बंधनों से आजादी दिलाते हैं, क्षणिक व सीमित दायरे में ही सही।
ReplyDeleteमुझे तो यह न्याय-व्यवस्था की समस्या लगती है। और इसे उसी तरह डील किया जाना चाहिये। नक्सली एक अलग तरह के माफिया हैं और वे भी गरीब जनता का अपने प्रकार से शोषण करते हैं।
ReplyDeleteउन्हे कठोर कदमों से कुचलना ही उपाय है।
आपकी बातें जायज है। पर अगर सरकारें इतनी संवेदनशील हो जाएं, तो फिर समाज में ये हाय हत्या क्यों रहे।
ReplyDelete-Zakir Ali ‘Rajnish’
{ Secretary-TSALIIM & SBAI }
नतीजे की चिंता किसे है ?हम -आप जैसे paagal sansad में नहीं baithhe huye .
ReplyDeletewaise jantaa tabhi तक surakshit है जब तक वह pulis पे bhrosaa नहीं kartee