हाय हम क्यों ऩा बिक़े-2
(दूसरी किश्त)
हरिशंकर राढ़ी
''हो सकता है कि आपकी बात ठीक हो, पर ऐसा पहले नहीं था। आजकल पतन थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। आज तो लोग-बाग खामखाह ही बिके जा रहे हैं।''
बोधनदास जी कुछ व्यंग्य पर उतर आए। मुझे लक्ष्य करके बोले, ''सरजी, किस जमाने की बात कर रहे हो ? कहाँ से शुरू करूँ ? किस युग का नाम पहले लूँ ? सतयुग ठीक रहेगा क्या ? आपको मालूम है कि सबसे बड़ा और सबसे पहले बिकने वाला आदमी कौन था? उसे खरीदा किसने था ?''
अब मैं चुप ! बिलकुल चुप ! ऐसा नहीं था कि मुझे कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था; मैं अपने आपको फंसता हुआ महसूस कर रहा था। मैंने नकारात्मक शैली में सिर हिलाया।
''भाई मेरे, मनुष्यों की बिक्री सतयुग से ही शुरू है। आप उससे अच्छे जमाने की कल्पना तो कर ही नहीं सकते ! आपको याद है कि सतयुग में अयोध्या के परम प्रतापी राजा हरिश्चंद्र बिके थे ? बिके क्या नीलाम ही हुए थे। हुए थे या नहीं ?''
इस बार तो जैसे मैं उछल ही पड़ा । मुझमें जान आ गई। मुझे लगा कि अब प्वाइंट मिल गया है जिसपर मैं इन्हें लथेड सकता हूँ। मैं उच्च स्वर में बोला, ''क्या बात करते हो अंकलजी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगुआ तेली ! सत्य हरिश्चंद्र की तुलना ? कहाँ वे और कहाँ ये आज के टुच्चे ? उन्होंने तो सत्य, धर्म और वचन की रक्षा के लिए पूरे परिवार का बलिदान कर दिया ।''
''तो उनके बिक जाने से कौन सा धर्म स्थापित हो गया ? जिस धर्म के लिए वे बिके थे, उसमें भी छल का ही प्रयोग किया गया था। आज भी लोग धर्म के नाम पर बिक रहे हैं और अपने को पता नहीं क्या-क्या समझ रहे हैं ! लोगों की तो बात छोड़ो, धर्म खुद ही बिक रहा है, सबसे ज्यादा बिक रहा है और वह भी डंके की चोट पर। फिर तुमने यह तो नहीं सोचा कि हरिश्चंद्र को खरीदने वाला कौन था? हरिश्चंद्र बिकता है तो उसे एक डोम खरीद लेता है जिसे यह भी नहीं पता कि हरिश्चंद्र की कीमत क्या है? कोई हो-हल्ला या हंगामा नहीं होता। कहानी सुनकर लोग आनन्दित हो लेते हैं, बस। अगर वहीं डोम बिकता और उसे हरिश्चंद्र खरीद लेते तो यह अलोकतांत्रिक और असामाजिक हो जाता। कितने तो पुतले फूँक दिए गए होते और 'हरिश्चंद्र ' नाम के कितने बेगुनाह पिट गए होते ? हरिश्चंद्र को खरीदने वाले डोम आज भी मानव बाजार पर कब्जा जमाए बैठे हैं। पहले के हरिश्चंद्र सत्य के लिए जरूर बिके थे किन्तु एक बार बिकने की परम्परा पड गई तो पड गई। पहले मनुष्य सत्य के लिए बिका, बाद में अर्थ और काम के लिए। रह गया मोक्ष, उसका तो कोई स्कोप ही नहीं।''
मुझे लगा कि मेरा दाँव खाली गया और बोधनदास जी यह प्रतियोगिता जीत जाएंगे। दरअसल मेरा 'राष्ट्रीय दर्द' अब एक प्रतियोगिता बन गया था और मैं इसे हारना नहीं चाहता था। मेरे हर नहले पर बोधनदास जी दहला लगाए जा रहे थे और मैं निरुत्तर होता जा रहा था। अब मेरे सामने एक ही रास्ता था कि क्यों न एक बुद्धिजीवी की भांति बाल की खाल निकालकर बात को उलझाया जाए और कम से कम बराबरी या अनिर्णय जैसी स्थिति में मामले को छोड़ा जाए। बहस जितनी ही उलझे, बुद्धिजीवी उतना ही बड़ा होता है। सो, मैंने कहा,'' देखिए, ये बात अलग है और आपने इसका गलत अर्थ निकाला है। सत्य हरिश्चंद्र का बिकना गर्व की बात है। ऐसे तो पता नहीं कितने लोग बिके हैं। मीराबाई ने तो कहा कि वे गिरिधर के हाथ बिकी हुई हैं। कबीरदास किसी 'रंगरेजवा' के हाथ बिके थे। कितने क्रान्तिकारी अपने देश के लिए बिक गए। ऐसे लोगों को यहाँ तुलना में भी खड़ा करना एक तरह से पाप होगा।''
''देखिए राढ़ी साहब, बाजार पाप और पुण्य के रेट से नहीं चलता। यह तो मुनाफे के दम पर चलता है, अर्थशास्त्र के सिद्धान्त पर चलता है। हाँ, इधर विज्ञापन के आधार पर भी चलने लगा है। पहले विज्ञापन नहीं था तो केवल मांग और आपूर्ति का नियम चलता था। एक बात और थी कि भाव क्रेता और विक्रेता की हैसियत के आधार पर भी तय होते थे। ग्राहक विदेशी हो तो पूछना ही क्या ? कुछ लोग तो विदेशी के हाथों बिकने को सौभाग्य मानते थे। स्वयं को इम्पोर्ट क्वालिटी का समझने लग जाते थे। विदेशी ग्राहक कीमत ऊँची लगाते थे और माल के साथ-साथ समय की भी कीमत समझते थे। देशी ग्राहकों की तरह वे भाव गिरने का इन्तजार नहीं करते थे।बल्कि आप यूँ भी कह सकते हैं कि वे गरम भाव का सामान खरीदना पसन्द करते थे। मीर जाफर की ही ले लो। सही समय पर सही ग्राहक के हाथ बिक गया। खुद के साथ-साथ देश को भी बेच दिया कि नहीं ? बस, कीमत सही लग गई थी। अब इतनी ऊँची कीमत कोई देशी डोम तो देने से रहा। आज मीर जाफर का भी नाम इतिहास में अमर है कि नहीं ? नियमतः तो अंगरेज बहादुर को उसके जन्मदिन पर छुट्टी रखनी चाहिए और उसकी जन्मशती मनानी चाहिए।''
मुझे लगा कि बोधनदास जी भी अब मेरे ही ट्रैक पर आ रहे हैं क्योंकि उनका स्वर व्यंग्यात्मक हो रहा था। मीर जाफर जैसे लोगों की बिक्री से वे भी आहत हैं। अब वे भी मान जाएँगे कि जिस तरह की मण्डी आजकल लग रही है, वह गलत है और इसपर हर देशवासी को विक्षुब्ध होना ही चाहिए। प्रकारान्तर से यह मेरे पक्ष की जीत है और मैं चाहता भी यही था। परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बोधनदास जी बढ़ते ही गए। आगे उन्होंने जारी रखा, ''और तुम्हें पता है कि यह परम्परा अभी भी जारी है। पहले तो एक ही मीर जाफर था, अब गिनती से परे हैं। कितने ही 'जिम्मेदार नागरिक' सेना और सुरक्षा की गोपनीय जानकारियाँ मुल्क को देकर उपकृत करते रहे और उपकृत होते रहे, तब तो तुम यह रोना कभी नहीं रोए कि आदमी बिका जा रहा है। दरअसल तुम बिक्री से आहत नहीं हो, तुम तो केवल विक्रयमूल्य से आहत हो। इन 'मीर जाफरों' की कीमत गोपनीय रही इसलिए तुम्हारा ध्यान गया ही नहीं ! आज जब एक खिलाडी दस करोड में बिक गया तो यह कीमत तुमसे हजम ही नहीं हुई ! ये तो कम से कम डंके की चोट पर नीलाम हो रहे हैं। मैंने पहले ही याद दिलाया कि दुनिया एक बाजार है और बिकने खरीदने का काम तो यहां चलता रहेगा। रह गई आदमी की बात तो वह तो सबसे बड़ा बिकाऊ माल है।''
अब मुझे अपनी पराजय बहुत निकट लगने लगी क्योंकि बोधनदास जी के तर्कों की काट मुझे कहीं भी नहीं मिल रही थी। मन ही मन मुझे अपनी गलती महसूस होने लगी थी। फिर भी मैंने मन मारकर आखिरी वार किया, ''अंकलजी, आपने तो थोड़ी ज्यादा ही फिलॉसफी झाड दी। माना कि कभी-कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि आदमी को बिकना पड जाए। मजबूरी की बात अलग है। कई तो अपना पेट भरने के लिए बिकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने किसी सगे-सम्बन्धी की दवा-दारू के लिए बिकने को तैयार हो जाते हैं। कुछ मजनूं टाइप के लोग 'प्यार' पर भी न्योछावर होकर मण्डी में बिकने आ जाते हैं। परन्तु एक अच्छे-खासे, खाते-पीते सुखी इंसान को बिकने की क्या जरूरत है? आपको नहीं लगता कि यह सब नैतिक पतन के कारण हो रहा है? इसके विरुद्ध समाज में आवाज नहीं उठनी चाहिए ?''बोधनदास जी बोले, ''श्रीमान राढ़ी साहब, किसी की जरूरत निश्चित करने का अधिकार आपको किसने दिया? बिकने वाले खुद को बेचने की आवश्यकता समझते हैं, तभी बिकते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि रेट बिकने वाले की आवश्यकता के स्तर से ही तय होते हैं। प्रश्न यह है कि आप स्वयं को किस उद्देश्य के तहत बेच रहे हैं? यदि आपकी आवश्यकता छोटी और घटिया है तो आपका रेट भी कम लगेगा। यदि आप भूखे हैं और खुद को रोटी के लिए नीलाम कर रहे हैं तो आपकी बोली भी रोटी की ही लगेगी। फिर आपका यह सोचना कि आपका भी भाव दस करोड हो जाए, नामुमकिन होगा। दवा-दारू के लिए खुद को बेच रहे हैं तो कीमत भी उसी हिसाब से तय होगी। अगर आप एक सुखी, वैभव शाली या फाइव स्टार जीवन की कल्पना करके बाजार में खड़े हैं तो कीमत भी फाइव स्टार की होगी। राढ़ी जी, देह का व्यापार बहुत पुराना है। इसी बाजार में एक देशी , कमसिन किन्तु हिन्दीभाषिणी नवयौवना का सुगठित शरीर दस-बीस रुपए में बिकता है क्योंकि वह रोटी का लक्ष्य लेकर पैदा होती है और इतने के लिए ही मण्डी में आती है; वहीं एक अर्धनग्न, बुढि या सी अंगरेजीभाषिणी रुपए में नहीं डॉलरों में बिकती है। उसकी आवश्यकता रोटी से कहीं ऊपर उठ चुकी है। उसे आत्मज्ञान हो चुका है, यानी वह अपने शरीर और बाजार की कीमत जानती है। अब आप स्वर्णबाजार छोड कर शाक बाज़ार में घूमेंगे तो आपकी कीमत तो शाक -भाजी की ही लगेगी न?
''फिर आज के बाजार में माल से ज्यादा रैपर की कीमत है। इस सत्य को जो नहीं पहचानेगा, वह रोटी के भाव ही बिकेगा। हिन्दी रैपर की चीज सस्ती बिकती है। इसके ग्राहकों की क्रय क्षमता और भावग्राह्यता ही कम होती है। वही शरीर अंगरेजी रैपर में लपेट दिया जाए तो फाइव स्टार श्रेणी का हो जाता है और कई बार तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का भी हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का भाव तो तुम्हें पता ही है। यह भी जानते ही होगे कि क्रिकेट का रैपर कितना शानदार है। अब तुम हॉकी या कबड्डी को ले लो। रैपर देशी है, ये रोटी के भाव भी नहीं बिकेंगे। हाँ, हम लोग किसी भाव नहीं बिक सके क्योंकि हम डिस्प्ले पर थे ही नहीं, स्वयं को कभी माल समझे ही नहीं। अब तो बस बाजार देखते जाओ और इसे एक मनोरंजन मानते रहो।''
मैं जैसे जमीन पर आ चुका था। आँखों के सामने वे सारे दृश्य घूम गए जब मैं बिक सकता था। बोधनदास एक विजयी योद्धा की भांति मुझे व्यर्थ का जीवनदान देकर जा चुके थे और मेरे मन में समस्त प्रश्नों का एकमात्र निचोड़ घूम रहा था- हाय, हम क्यों ना बिके ?
''हो सकता है कि आपकी बात ठीक हो, पर ऐसा पहले नहीं था। आजकल पतन थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। आज तो लोग-बाग खामखाह ही बिके जा रहे हैं।''
बोधनदास जी कुछ व्यंग्य पर उतर आए। मुझे लक्ष्य करके बोले, ''सरजी, किस जमाने की बात कर रहे हो ? कहाँ से शुरू करूँ ? किस युग का नाम पहले लूँ ? सतयुग ठीक रहेगा क्या ? आपको मालूम है कि सबसे बड़ा और सबसे पहले बिकने वाला आदमी कौन था? उसे खरीदा किसने था ?''
अब मैं चुप ! बिलकुल चुप ! ऐसा नहीं था कि मुझे कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था; मैं अपने आपको फंसता हुआ महसूस कर रहा था। मैंने नकारात्मक शैली में सिर हिलाया।
''भाई मेरे, मनुष्यों की बिक्री सतयुग से ही शुरू है। आप उससे अच्छे जमाने की कल्पना तो कर ही नहीं सकते ! आपको याद है कि सतयुग में अयोध्या के परम प्रतापी राजा हरिश्चंद्र बिके थे ? बिके क्या नीलाम ही हुए थे। हुए थे या नहीं ?''
इस बार तो जैसे मैं उछल ही पड़ा । मुझमें जान आ गई। मुझे लगा कि अब प्वाइंट मिल गया है जिसपर मैं इन्हें लथेड सकता हूँ। मैं उच्च स्वर में बोला, ''क्या बात करते हो अंकलजी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगुआ तेली ! सत्य हरिश्चंद्र की तुलना ? कहाँ वे और कहाँ ये आज के टुच्चे ? उन्होंने तो सत्य, धर्म और वचन की रक्षा के लिए पूरे परिवार का बलिदान कर दिया ।''
''तो उनके बिक जाने से कौन सा धर्म स्थापित हो गया ? जिस धर्म के लिए वे बिके थे, उसमें भी छल का ही प्रयोग किया गया था। आज भी लोग धर्म के नाम पर बिक रहे हैं और अपने को पता नहीं क्या-क्या समझ रहे हैं ! लोगों की तो बात छोड़ो, धर्म खुद ही बिक रहा है, सबसे ज्यादा बिक रहा है और वह भी डंके की चोट पर। फिर तुमने यह तो नहीं सोचा कि हरिश्चंद्र को खरीदने वाला कौन था? हरिश्चंद्र बिकता है तो उसे एक डोम खरीद लेता है जिसे यह भी नहीं पता कि हरिश्चंद्र की कीमत क्या है? कोई हो-हल्ला या हंगामा नहीं होता। कहानी सुनकर लोग आनन्दित हो लेते हैं, बस। अगर वहीं डोम बिकता और उसे हरिश्चंद्र खरीद लेते तो यह अलोकतांत्रिक और असामाजिक हो जाता। कितने तो पुतले फूँक दिए गए होते और 'हरिश्चंद्र ' नाम के कितने बेगुनाह पिट गए होते ? हरिश्चंद्र को खरीदने वाले डोम आज भी मानव बाजार पर कब्जा जमाए बैठे हैं। पहले के हरिश्चंद्र सत्य के लिए जरूर बिके थे किन्तु एक बार बिकने की परम्परा पड गई तो पड गई। पहले मनुष्य सत्य के लिए बिका, बाद में अर्थ और काम के लिए। रह गया मोक्ष, उसका तो कोई स्कोप ही नहीं।''
मुझे लगा कि मेरा दाँव खाली गया और बोधनदास जी यह प्रतियोगिता जीत जाएंगे। दरअसल मेरा 'राष्ट्रीय दर्द' अब एक प्रतियोगिता बन गया था और मैं इसे हारना नहीं चाहता था। मेरे हर नहले पर बोधनदास जी दहला लगाए जा रहे थे और मैं निरुत्तर होता जा रहा था। अब मेरे सामने एक ही रास्ता था कि क्यों न एक बुद्धिजीवी की भांति बाल की खाल निकालकर बात को उलझाया जाए और कम से कम बराबरी या अनिर्णय जैसी स्थिति में मामले को छोड़ा जाए। बहस जितनी ही उलझे, बुद्धिजीवी उतना ही बड़ा होता है। सो, मैंने कहा,'' देखिए, ये बात अलग है और आपने इसका गलत अर्थ निकाला है। सत्य हरिश्चंद्र का बिकना गर्व की बात है। ऐसे तो पता नहीं कितने लोग बिके हैं। मीराबाई ने तो कहा कि वे गिरिधर के हाथ बिकी हुई हैं। कबीरदास किसी 'रंगरेजवा' के हाथ बिके थे। कितने क्रान्तिकारी अपने देश के लिए बिक गए। ऐसे लोगों को यहाँ तुलना में भी खड़ा करना एक तरह से पाप होगा।''
''देखिए राढ़ी साहब, बाजार पाप और पुण्य के रेट से नहीं चलता। यह तो मुनाफे के दम पर चलता है, अर्थशास्त्र के सिद्धान्त पर चलता है। हाँ, इधर विज्ञापन के आधार पर भी चलने लगा है। पहले विज्ञापन नहीं था तो केवल मांग और आपूर्ति का नियम चलता था। एक बात और थी कि भाव क्रेता और विक्रेता की हैसियत के आधार पर भी तय होते थे। ग्राहक विदेशी हो तो पूछना ही क्या ? कुछ लोग तो विदेशी के हाथों बिकने को सौभाग्य मानते थे। स्वयं को इम्पोर्ट क्वालिटी का समझने लग जाते थे। विदेशी ग्राहक कीमत ऊँची लगाते थे और माल के साथ-साथ समय की भी कीमत समझते थे। देशी ग्राहकों की तरह वे भाव गिरने का इन्तजार नहीं करते थे।बल्कि आप यूँ भी कह सकते हैं कि वे गरम भाव का सामान खरीदना पसन्द करते थे। मीर जाफर की ही ले लो। सही समय पर सही ग्राहक के हाथ बिक गया। खुद के साथ-साथ देश को भी बेच दिया कि नहीं ? बस, कीमत सही लग गई थी। अब इतनी ऊँची कीमत कोई देशी डोम तो देने से रहा। आज मीर जाफर का भी नाम इतिहास में अमर है कि नहीं ? नियमतः तो अंगरेज बहादुर को उसके जन्मदिन पर छुट्टी रखनी चाहिए और उसकी जन्मशती मनानी चाहिए।''
मुझे लगा कि बोधनदास जी भी अब मेरे ही ट्रैक पर आ रहे हैं क्योंकि उनका स्वर व्यंग्यात्मक हो रहा था। मीर जाफर जैसे लोगों की बिक्री से वे भी आहत हैं। अब वे भी मान जाएँगे कि जिस तरह की मण्डी आजकल लग रही है, वह गलत है और इसपर हर देशवासी को विक्षुब्ध होना ही चाहिए। प्रकारान्तर से यह मेरे पक्ष की जीत है और मैं चाहता भी यही था। परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बोधनदास जी बढ़ते ही गए। आगे उन्होंने जारी रखा, ''और तुम्हें पता है कि यह परम्परा अभी भी जारी है। पहले तो एक ही मीर जाफर था, अब गिनती से परे हैं। कितने ही 'जिम्मेदार नागरिक' सेना और सुरक्षा की गोपनीय जानकारियाँ मुल्क को देकर उपकृत करते रहे और उपकृत होते रहे, तब तो तुम यह रोना कभी नहीं रोए कि आदमी बिका जा रहा है। दरअसल तुम बिक्री से आहत नहीं हो, तुम तो केवल विक्रयमूल्य से आहत हो। इन 'मीर जाफरों' की कीमत गोपनीय रही इसलिए तुम्हारा ध्यान गया ही नहीं ! आज जब एक खिलाडी दस करोड में बिक गया तो यह कीमत तुमसे हजम ही नहीं हुई ! ये तो कम से कम डंके की चोट पर नीलाम हो रहे हैं। मैंने पहले ही याद दिलाया कि दुनिया एक बाजार है और बिकने खरीदने का काम तो यहां चलता रहेगा। रह गई आदमी की बात तो वह तो सबसे बड़ा बिकाऊ माल है।''
अब मुझे अपनी पराजय बहुत निकट लगने लगी क्योंकि बोधनदास जी के तर्कों की काट मुझे कहीं भी नहीं मिल रही थी। मन ही मन मुझे अपनी गलती महसूस होने लगी थी। फिर भी मैंने मन मारकर आखिरी वार किया, ''अंकलजी, आपने तो थोड़ी ज्यादा ही फिलॉसफी झाड दी। माना कि कभी-कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि आदमी को बिकना पड जाए। मजबूरी की बात अलग है। कई तो अपना पेट भरने के लिए बिकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने किसी सगे-सम्बन्धी की दवा-दारू के लिए बिकने को तैयार हो जाते हैं। कुछ मजनूं टाइप के लोग 'प्यार' पर भी न्योछावर होकर मण्डी में बिकने आ जाते हैं। परन्तु एक अच्छे-खासे, खाते-पीते सुखी इंसान को बिकने की क्या जरूरत है? आपको नहीं लगता कि यह सब नैतिक पतन के कारण हो रहा है? इसके विरुद्ध समाज में आवाज नहीं उठनी चाहिए ?''बोधनदास जी बोले, ''श्रीमान राढ़ी साहब, किसी की जरूरत निश्चित करने का अधिकार आपको किसने दिया? बिकने वाले खुद को बेचने की आवश्यकता समझते हैं, तभी बिकते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि रेट बिकने वाले की आवश्यकता के स्तर से ही तय होते हैं। प्रश्न यह है कि आप स्वयं को किस उद्देश्य के तहत बेच रहे हैं? यदि आपकी आवश्यकता छोटी और घटिया है तो आपका रेट भी कम लगेगा। यदि आप भूखे हैं और खुद को रोटी के लिए नीलाम कर रहे हैं तो आपकी बोली भी रोटी की ही लगेगी। फिर आपका यह सोचना कि आपका भी भाव दस करोड हो जाए, नामुमकिन होगा। दवा-दारू के लिए खुद को बेच रहे हैं तो कीमत भी उसी हिसाब से तय होगी। अगर आप एक सुखी, वैभव शाली या फाइव स्टार जीवन की कल्पना करके बाजार में खड़े हैं तो कीमत भी फाइव स्टार की होगी। राढ़ी जी, देह का व्यापार बहुत पुराना है। इसी बाजार में एक देशी , कमसिन किन्तु हिन्दीभाषिणी नवयौवना का सुगठित शरीर दस-बीस रुपए में बिकता है क्योंकि वह रोटी का लक्ष्य लेकर पैदा होती है और इतने के लिए ही मण्डी में आती है; वहीं एक अर्धनग्न, बुढि या सी अंगरेजीभाषिणी रुपए में नहीं डॉलरों में बिकती है। उसकी आवश्यकता रोटी से कहीं ऊपर उठ चुकी है। उसे आत्मज्ञान हो चुका है, यानी वह अपने शरीर और बाजार की कीमत जानती है। अब आप स्वर्णबाजार छोड कर शाक बाज़ार में घूमेंगे तो आपकी कीमत तो शाक -भाजी की ही लगेगी न?
''फिर आज के बाजार में माल से ज्यादा रैपर की कीमत है। इस सत्य को जो नहीं पहचानेगा, वह रोटी के भाव ही बिकेगा। हिन्दी रैपर की चीज सस्ती बिकती है। इसके ग्राहकों की क्रय क्षमता और भावग्राह्यता ही कम होती है। वही शरीर अंगरेजी रैपर में लपेट दिया जाए तो फाइव स्टार श्रेणी का हो जाता है और कई बार तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का भी हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का भाव तो तुम्हें पता ही है। यह भी जानते ही होगे कि क्रिकेट का रैपर कितना शानदार है। अब तुम हॉकी या कबड्डी को ले लो। रैपर देशी है, ये रोटी के भाव भी नहीं बिकेंगे। हाँ, हम लोग किसी भाव नहीं बिक सके क्योंकि हम डिस्प्ले पर थे ही नहीं, स्वयं को कभी माल समझे ही नहीं। अब तो बस बाजार देखते जाओ और इसे एक मनोरंजन मानते रहो।''
मैं जैसे जमीन पर आ चुका था। आँखों के सामने वे सारे दृश्य घूम गए जब मैं बिक सकता था। बोधनदास एक विजयी योद्धा की भांति मुझे व्यर्थ का जीवनदान देकर जा चुके थे और मेरे मन में समस्त प्रश्नों का एकमात्र निचोड़ घूम रहा था- हाय, हम क्यों ना बिके ?




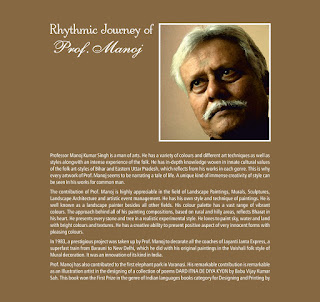


very very nice :)
ReplyDelete----
अपनी रचनाओं का कॉपीराइट मुफ़्त पाइए
आज के बाजार में माल से ज्यादा रैपर की कीमत है।
ReplyDeleteबहुत खुबसूरत , सोचने को विवश करती रचना, आभार
'समकालीन अभिव्यक्ति में छपने के लिए बधाई ....!!
ReplyDelete