भारतीय इतिहास पर एसिड अटैक
इष्ट देव सांकृत्यायन
अगर भंसाली ने अपनी फिल्म में ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश की है, जैसा बताया जा रहा है तो इसे क्या माना जाए? यह भारतीय इतिहास के स्थापित तथ्यों के साथ खिलवाड़ नहीं, बलात्कार जैसा है. इतिहास के सीने में खंजर भोंकने जैसा है. क्या दुनिया का कोई और देश अपने इतिहास के स्थापित तथ्यों के साथ कला के नाम पर ऐसा कुछ करने की इजाजत देता है? भारतीय इतिहास और जन ऐसी इजाजत क्यों देगा? उससे यह मूर्खतापूर्ण अपेक्षा क्यों की जानी चाहिए? क्या यह वैसा ही जघन्य अपराध नहीं है जैसे बलात्कार या छेड़छाड़ के किसी मामले में अपराधी को उसके अत्याचारों की शिकार लड़की का प्रेमी बताया जाए? क्या यह् पद्मावती की चरित्र हत्या जैसा मामला नहीं है? यह कौन करता है? वे टुच्चे वकील जिनका पेशा ऐसे घटिया लोगों की पक्षधरता करके ही चलता है. जिनके बारे में माना जाता है कि नैतिकता, मानवता और जीवन के उदात्त मूल्यों से उनका कोई लेना-देना नहीं है. क्या कला का धंधा करने वाले उन वकीलों से भी ज़्यादा गए-गुज़रे हो गए हैं? क्या इनका कोई दीन-ईमान नहीं रह गया है? क्या यह न केवल भारतीय इतिहास, बल्कि भारतीय जन से भी विश्वासघात जैसा नहीं है? क्या कला इसीलिए होती है?
भारतीय इतिहास पर एसिड अटैक का यह दौर बहुत लंबे समय से चला आ रहा है. यह बार-बार समय और जगह बदल-बदल कर भिन्न-भिन्न रूपों में होता आ रहा है. सही कहें तो इस प्रवृत्ति को पिछले 70 वर्षों में सत्ता प्रतिष्ठान ने जान-बूझकर बढ़ावा दिया है. एक समुदाय के मिथकों-प्रतीकों के साथ जब भी कुछ बेहूदी हरकत की गई तो उसके विरोध को ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन’ बताकर लगभग बर्बरता से दबा दिया गया. यहाँ तक कि एक टुच्चा पेंटर बार-बार अदालत के सम्मन की अनदेखी करता रहा और जब उसके ख़िलाफ़ वारंट कट गया तो इसे इमरजेंसी से भी भयावह बताया गया. क्या यह वही मानसिकता नहीं है जो ‘अफ़जल हम शर्मिंदा हैं/तेरे क़ातिल ज़िंदा हैं’ का नारा लगाते हुए देश के माननीय उच्चतम न्यायालय को क़ातिल बताने में भी संकोच नहीं करती? उस पर तुर्रा ये कि यही संविधान में सबसे बड़े आस्था रखने वाले भी हैं. बाक़ी लोग संविधान की ऐसी-तैसी कर रहे हैं. यह बताने वाले वही लोग थे जिन्हें तसलीमा नसरीन, सलमान रुश्दी, एम.ए.खान, तारिक़ फ़तह, हसन निसार के नाम पर साँप सूँघ जाता है. वहीं दूसरी ओर शर्ले एब्दो की घटना पर चुप्पी साध ली गई. क्यों?
उस ख़ास वर्ग की यह चुप्पी बहुत दिनों तक सधी नहीं रही. थोड़े दिनों बाद जब हल्ला थम गया तो मुखर हुई और मुखर इस रूप में हुई कि ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कोई तो सीमा होनी चाहिए’. फेसबुक-ट्विटर पर इस तरह की अभिव्यक्तियों की भरमार हो गई. यह सीमाएँ बताने वाले भी वही थे, जो एक टुच्चे पेंटर के मामले में अभिव्यक्ति की अनंत स्वतंत्रता के बड़े भारी पैरोकार बने फिर रहे थे. क्या इस मानसिकता को आप ‘दोगली’ के अलावा कोई और संज्ञा दे सकते हैं?
उस ख़ास समुदाय के ही संबंध में इन्हें सीमाएँ क्यों याद आती हैं? केवल इसलिए न कि वह इनकी उस चक्रव्यूह रूपी चुनौती के षड्यंत्र को स्वीकार नहीं करता जिसे ये संवाद या बहस या विमर्श कहते हैं! वह बात करने की एक ही भाषा जानता है और वह है बंदूक. जो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं उन्हें ये पहले तो दकियानूस करार देते हैं और फिर बहस का मैदान छोड़कर भाग जाते हैं. अपनी एक ख़ास खोल में छिपे हुए वहीं से भौं-भौं करते रहते हैं. ग़लती से कोई इनका सुरक्षा घेरा तोड़कर भीतर घुस गया और वहाँ इनसे बहस करने बैठ गया तो पहले तो उसके तथ्यगत सही तर्कों को सुनने से ही इनकार कर देते हैं और फिर उस पर कुतर्कों की बौछार कर देते हैं. इस पर भी कुछ रह गया तो देश भर के अख़बारों-टीवी चैनलों में रंगे सियारों की तरह हुआँ-हुआँ शुरू कर देते हैं. इसके बाद चारा क्या बचता है?
साहित्य में यह बात बार-बार कही जाती रही है कि ऐतिहासिक उपन्यास इतिहास नहीं होता. लेकिन साथ ही यह भी कहा जाता रहा है कि ऐतिहासिक उपन्यास की अपनी सीमाएँ होती हैं. साफ़ अर्थ है कि साहित्य में कल्पना के पुट के नाम पर इतिहास के तथ्यों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता. इसकी अनुमति स्वयं साहित्य भी नहीं देता. ऐसा केवल हिंदी या भारतीय साहित्य में नहीं है, दुनिया भर का साहित्य इस धारणा को मान्यता देता है. वह इस धारणा को मान्यता इसलिए देता है क्योंकि अगर ऐसा न किया गया तो साहित्य और इतिहास के बीच बड़ी अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी. जो न तो साहित्य के लिए ठीक होगी, न इतिहास के लिए और न ही समाज के लिए. इसके बावजूद भारतीय साहित्य में ऐसी छूट ली गई है और वह छूट लेने वाले कोई दूसरे नहीं, वही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर साहित्य को अपनी कुंठाओं का उगालदान बनाने वाले हैं. आज वही गिरोह है जो सिनेमा में करोड़ों की लागत लगाकर अरबों का मुनाफ़ा कमाने वाले ग़रीब संजय लीला भंसाली के पीछे एक बार फिर खड़ा हो गया है. क्या अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य की इस पैरोकारी और इस कलावाद पर आपको हँसी नहीं आती?
मुझे सिनेमा को इतिहास संबंधी अपनी कुंठाओं का उगालदान बनाने वालों पर जूते पड़ने का कोई अफ़सोस नहीं है. हाँ, अफ़सोस इस बात का है कि ये जूते मारने वाले अभी तक या तो केवल क्षणिक आवेश के शिकार साबित हुए हैं या फिर भाड़े के कुत्ते. जो अंततः इन ग़रीब खरबपतियों के लिए मुनाफ़ा बढ़ाने वाले औजार ही साबित होते हैं. अगर करणी सेना इसे इतिहास और स्त्री की अस्मिता के साथ खिलवाड़ का मामला बनाकर अदालत तक न ले गई और अदालत से यह फिल्म बनने पर रोक न लगवा सकी तो उसे भी भाड़े का कुत्ता ही माना जाएगा.
अगर भंसाली ने अपनी फिल्म में ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश की है, जैसा बताया जा रहा है तो इसे क्या माना जाए? यह भारतीय इतिहास के स्थापित तथ्यों के साथ खिलवाड़ नहीं, बलात्कार जैसा है. इतिहास के सीने में खंजर भोंकने जैसा है. क्या दुनिया का कोई और देश अपने इतिहास के स्थापित तथ्यों के साथ कला के नाम पर ऐसा कुछ करने की इजाजत देता है? भारतीय इतिहास और जन ऐसी इजाजत क्यों देगा? उससे यह मूर्खतापूर्ण अपेक्षा क्यों की जानी चाहिए? क्या यह वैसा ही जघन्य अपराध नहीं है जैसे बलात्कार या छेड़छाड़ के किसी मामले में अपराधी को उसके अत्याचारों की शिकार लड़की का प्रेमी बताया जाए? क्या यह् पद्मावती की चरित्र हत्या जैसा मामला नहीं है? यह कौन करता है? वे टुच्चे वकील जिनका पेशा ऐसे घटिया लोगों की पक्षधरता करके ही चलता है. जिनके बारे में माना जाता है कि नैतिकता, मानवता और जीवन के उदात्त मूल्यों से उनका कोई लेना-देना नहीं है. क्या कला का धंधा करने वाले उन वकीलों से भी ज़्यादा गए-गुज़रे हो गए हैं? क्या इनका कोई दीन-ईमान नहीं रह गया है? क्या यह न केवल भारतीय इतिहास, बल्कि भारतीय जन से भी विश्वासघात जैसा नहीं है? क्या कला इसीलिए होती है?
भारतीय इतिहास पर एसिड अटैक का यह दौर बहुत लंबे समय से चला आ रहा है. यह बार-बार समय और जगह बदल-बदल कर भिन्न-भिन्न रूपों में होता आ रहा है. सही कहें तो इस प्रवृत्ति को पिछले 70 वर्षों में सत्ता प्रतिष्ठान ने जान-बूझकर बढ़ावा दिया है. एक समुदाय के मिथकों-प्रतीकों के साथ जब भी कुछ बेहूदी हरकत की गई तो उसके विरोध को ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन’ बताकर लगभग बर्बरता से दबा दिया गया. यहाँ तक कि एक टुच्चा पेंटर बार-बार अदालत के सम्मन की अनदेखी करता रहा और जब उसके ख़िलाफ़ वारंट कट गया तो इसे इमरजेंसी से भी भयावह बताया गया. क्या यह वही मानसिकता नहीं है जो ‘अफ़जल हम शर्मिंदा हैं/तेरे क़ातिल ज़िंदा हैं’ का नारा लगाते हुए देश के माननीय उच्चतम न्यायालय को क़ातिल बताने में भी संकोच नहीं करती? उस पर तुर्रा ये कि यही संविधान में सबसे बड़े आस्था रखने वाले भी हैं. बाक़ी लोग संविधान की ऐसी-तैसी कर रहे हैं. यह बताने वाले वही लोग थे जिन्हें तसलीमा नसरीन, सलमान रुश्दी, एम.ए.खान, तारिक़ फ़तह, हसन निसार के नाम पर साँप सूँघ जाता है. वहीं दूसरी ओर शर्ले एब्दो की घटना पर चुप्पी साध ली गई. क्यों?
उस ख़ास वर्ग की यह चुप्पी बहुत दिनों तक सधी नहीं रही. थोड़े दिनों बाद जब हल्ला थम गया तो मुखर हुई और मुखर इस रूप में हुई कि ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कोई तो सीमा होनी चाहिए’. फेसबुक-ट्विटर पर इस तरह की अभिव्यक्तियों की भरमार हो गई. यह सीमाएँ बताने वाले भी वही थे, जो एक टुच्चे पेंटर के मामले में अभिव्यक्ति की अनंत स्वतंत्रता के बड़े भारी पैरोकार बने फिर रहे थे. क्या इस मानसिकता को आप ‘दोगली’ के अलावा कोई और संज्ञा दे सकते हैं?
उस ख़ास समुदाय के ही संबंध में इन्हें सीमाएँ क्यों याद आती हैं? केवल इसलिए न कि वह इनकी उस चक्रव्यूह रूपी चुनौती के षड्यंत्र को स्वीकार नहीं करता जिसे ये संवाद या बहस या विमर्श कहते हैं! वह बात करने की एक ही भाषा जानता है और वह है बंदूक. जो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं उन्हें ये पहले तो दकियानूस करार देते हैं और फिर बहस का मैदान छोड़कर भाग जाते हैं. अपनी एक ख़ास खोल में छिपे हुए वहीं से भौं-भौं करते रहते हैं. ग़लती से कोई इनका सुरक्षा घेरा तोड़कर भीतर घुस गया और वहाँ इनसे बहस करने बैठ गया तो पहले तो उसके तथ्यगत सही तर्कों को सुनने से ही इनकार कर देते हैं और फिर उस पर कुतर्कों की बौछार कर देते हैं. इस पर भी कुछ रह गया तो देश भर के अख़बारों-टीवी चैनलों में रंगे सियारों की तरह हुआँ-हुआँ शुरू कर देते हैं. इसके बाद चारा क्या बचता है?
साहित्य में यह बात बार-बार कही जाती रही है कि ऐतिहासिक उपन्यास इतिहास नहीं होता. लेकिन साथ ही यह भी कहा जाता रहा है कि ऐतिहासिक उपन्यास की अपनी सीमाएँ होती हैं. साफ़ अर्थ है कि साहित्य में कल्पना के पुट के नाम पर इतिहास के तथ्यों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता. इसकी अनुमति स्वयं साहित्य भी नहीं देता. ऐसा केवल हिंदी या भारतीय साहित्य में नहीं है, दुनिया भर का साहित्य इस धारणा को मान्यता देता है. वह इस धारणा को मान्यता इसलिए देता है क्योंकि अगर ऐसा न किया गया तो साहित्य और इतिहास के बीच बड़ी अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी. जो न तो साहित्य के लिए ठीक होगी, न इतिहास के लिए और न ही समाज के लिए. इसके बावजूद भारतीय साहित्य में ऐसी छूट ली गई है और वह छूट लेने वाले कोई दूसरे नहीं, वही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर साहित्य को अपनी कुंठाओं का उगालदान बनाने वाले हैं. आज वही गिरोह है जो सिनेमा में करोड़ों की लागत लगाकर अरबों का मुनाफ़ा कमाने वाले ग़रीब संजय लीला भंसाली के पीछे एक बार फिर खड़ा हो गया है. क्या अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य की इस पैरोकारी और इस कलावाद पर आपको हँसी नहीं आती?
मुझे सिनेमा को इतिहास संबंधी अपनी कुंठाओं का उगालदान बनाने वालों पर जूते पड़ने का कोई अफ़सोस नहीं है. हाँ, अफ़सोस इस बात का है कि ये जूते मारने वाले अभी तक या तो केवल क्षणिक आवेश के शिकार साबित हुए हैं या फिर भाड़े के कुत्ते. जो अंततः इन ग़रीब खरबपतियों के लिए मुनाफ़ा बढ़ाने वाले औजार ही साबित होते हैं. अगर करणी सेना इसे इतिहास और स्त्री की अस्मिता के साथ खिलवाड़ का मामला बनाकर अदालत तक न ले गई और अदालत से यह फिल्म बनने पर रोक न लगवा सकी तो उसे भी भाड़े का कुत्ता ही माना जाएगा.




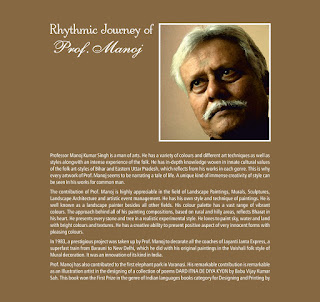


बढ़िया
ReplyDeleteThis is the precise weblog for anybody who needs to seek out out about this topic. You notice so much its almost arduous to argue with you. You positively put a brand new spin on a subject that's been written about for years. Nice stuff, simply nice!
ReplyDeleteThanks for appreciation sir!
Deleteदेखा. आभार.
ReplyDeleteबढ़िया
ReplyDelete