नाम में क्या नहीं रक्खा!
हाल ही में मार्क जुकरबर्ग
ने अपनी बहन रैंडी जुकरबर्ग को किसी उपलब्धि पर बधाई दी थी। इसके तुरंत बाद ही रैंडी
के नाम का अपने हिसाब से देसी अर्थ निकालकर भाई लोग पिल पड़े। केवल भारत नहीं, पूरा दक्षिण एशिया शामिल था उनमें। खैर, अच्छी बात रही कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद वे
जानते हैं कि इतिहास जो भी रहा हो, आज का सच यह है कि एशियाई समाज एक यौन कुंठित समाज है।
और तो जाने दीजिए, हम भारत के भीतर ही कई बार ऐसा करते हैं। पंजाब के कुछ नाम
उत्तर प्रदेश, बिहार
या मध्य प्रदेश में कुछ अन्यथा अर्थ देते हैं। ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश के नाम पंजाब या तमिलनाडु में भी। यह
स्थानीय बोलियों और भाषाओं में शब्दों की अर्थ-छवियों के वैविध्य का परिणाम है। जो
एक बार पूरा भारत घूम लेता है, वह
इससे सहज हो जाता है। एक जगह में सिमटा व्यक्ति ऐसे ही बार-बार हैरत में पड़ता रहता
है।
इसी क्रम में एक और
बात होती है, नामों
को धर्म से जोड़कर देखना। ऐसे तो नामों का किसी धार्मिक पंथविशेष से कुछ लेना-देना है
नहीं। क्योंकि नाम संज्ञा हैं और संज्ञाएं शब्द हैं। शब्द किसी भाषाविशेष के होते हैं।
भाषाएं क्षेत्रविशेष की होती हैं। अपने दायरे में व्यक्ति को व्यक्ति और उससे बाहर
निकलकर एक समाज या समुदाय को दूसरे समाज या समुदाय से जोड़ने वाली। भाषाएं एक संस्कृति
का अंग होती हैं और संस्कृति के ही अंग होते हैं धर्म या पंथ। किसी धर्म या पंथ का
अंग संस्कृति नहीं है, न
ऐसा हो सकता है। किसी भाषा या संस्कृति को किसी पंथ का अंग बना देना वैसे ही है जैसे ब्रह्मांड को किसी ग्रह का अंग बना देना। यह कोशिश ही
प्रलय को निमंत्रण है।
भारत में लंबे समय तक
विदेशी दासता और खासकर अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति का शिकार होने का परिणाम
यह हुआ है कि भाषाओं को पंथों से जोड़ने की कोशिश होने लगी। इसके सफलता या विफलता पर
कुछ कहना यहाँ समीचीन नहीं होगा। लेकिन इतना तो हुआ है कि नाम हिंदू और मुसलमान होने लगे। हमारे लोग इंडोनेशिया के नामों पर गौर
करें, जिनका राजकीय पंथ इस्लाम है, तो उन्हें आश्चर्य होगा। कुछ ऐसा ही कश्मीर के बारे में है।
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य
प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा के लोग
जब कश्मीर में अरबी-फारसी संज्ञाओं के साथ संस्कृत या हिंदू उपनाम और संस्कृत-हिंदी
संज्ञाओं के साथ मुस्लिम उपनाम पढ़ते सुनते हैं तो थोड़ा अचरज होता है। यहाँ दिल्ली में
जब लोग इरफान अभय पंडित जैसे सुनील अहमद टिकू जैसे नाम सुनते हैं तो कई बार उन्हें
लगता है कि यह शायद सामंजस्य बिठाने का प्रयास है, इस्लामी कट्टरता से। पहली बार जब मैं वहाँ गया था, सन 2000 में तो मुझे भी असमंजस हुआ था। लेकिन पूरी घुमक्कड़ी
और उनके रीति-रिवाज एवं परंपराओं से रूबरू होने के बाद अचरज और असमंजस ही नहीं जाता
रहा, एक प्रीतिकर एहसास हुआ।
कश्मीर में ऋषियों की
एक ऐसी परंपरा है जो मुसलमानों में सूफी संतों के रूप में माने जाते हैं और सूफियों
की एक ऐसी परंपरा है जो हिंदुओं में ऋषियों के रूप में प्रतिष्ठित हैं। एक ही व्यक्ति
दो अलग-अलग संप्रदायों में दो अलग-अलग नामों से सम्मानित-प्रतिष्ठित है और यह सब जानते-समझते
हुए। लाख साजिशों के बावजूद न तो अब्दुल्ला-मुफ्ती की सरकारें इसे तोड़ पाईं, न बरास्ता पाकिस्तान आया अरबी वहाबवाद, न पाकिस्तान-आइएसआइ फंडेड और स्थानीय अलगाववादियों द्वारा
पोषित आतंकवाद, न
मस्जिदों से फैलाई गई अति हिंसक कड़वाहट और न उससे आजिज आकर अपना घर-बार सब छोड़कर दर-बदर
हो गए हिंदुओं के मन में अपने ही कुछ पड़ोसियों के प्रति मन में उपजी दरारें।
ऐसा नहीं है कि यह केवल
हिंदुओं में ही है। कश्मीर के ज्यादातर मुसलमानों के साथ भी ऐसा ही है। अब्दुल्ला और
मुफ्ती के शासन को मुसलमानों में मान्य ऋषियों के प्रति उनकी श्रद्धा को कम करने में
जब कोई सफलता नहीं मिली तो उन्होंने उनकी मुसलिम पहचानों पर जोर देना शुरू कर दिया।
मुसलमानों को इस बात के लिए लगभग मजबूर किया गया कि वे उनके वही नाम याद रखें जो सरकारें
चाहती हैं।
यही बात कई जगहों के
मामले में हुई। स्थानीय स्तर पर ही ज्ञात कई पहाड़ों और झीलों के नाम बदले गए। उन्हें
बार-बार स्थानीय मुसलमानों के मन में स्थापित करने की कोशिश की गई। वे भारतीयता से
जुड़ाव की अपनी सारी पहचानें भूल जाएं, इसकी हर संभव साजिश 370 और 35 क
की आड़ में हुई। हालांकि न तो उसे वह भूला और भूलने वाला है।
ऊपर से थोपे गए अलगाववाद
को ऋषियों और सूफी संतों की जिस उदात्त परंपरा ने ज़मीन पर कभी अंकुरित ही नहीं होने
दिया, उसके कुछ अनमोल हीरों का जिक्र
अगली कड़ी में।
©इष्ट देव
सांकृत्यायन




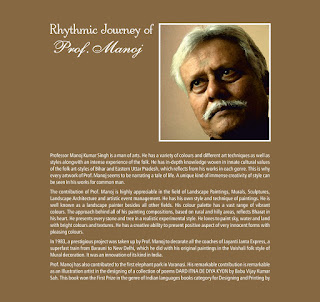


Comments
Post a Comment
सुस्वागतम!!