हिंदी वालों का दंभ और समाज में उनकी भूमिका
इष्ट देव सांकृत्यायन
60 के बाद की जो हिंदी है, दंभ से उसका चोली-दामन का साथ है। क्योंकि 47 में जो संविधान सभा के बहुमत के बावजूद हिंदी के राष्ट्रभाषा बनाए जाने का विरोध कर रहे थे और आखिरकार उसे अपने षड्यनत्रकारी दुष्चक्र में फँसाकर राजभाषा के दायरे में सीमित कर ही डाला, उन्होंने ही अपने उसी षड्यंत्र चातुर्य का उपयोग कर हिंदी की छाती पर अपने वर्चस्व का खूँटा गाड़ लिया। यह किस एक महापुरुष की कृपा का फल है, इस पर बार-बार बोलने का कोई लाभ नहीं।
लेकिन जब बात समाज को बचाने में साहित्य की भूमिका
की आएगी तो उन्हीं दंभियों में से कई अपनी वे कीलें ले-लेकर निकल आएंगे जो
उन्होंने कभी हिंदी सेवा के नाम पर हिंदी भाषा, साहित्य और समाज के
चक्के में ठोंकी थीं। उन्होंने वे कीलें ठोंकी तो थीं हिंदी के चक्के की हवा
निकालने के लिए,
लेकिन सहस्राब्दियों से वंचित समाज की अंतर्निहित
चेतना ने उसका भी उपयोग कर लिया। वह उपयोग उसने अपनी मजबूती बढ़ाने में किया।
आखिरकार गाड़ी और ज्यादा मजबूती से समय की सड़क पर जम गई और बेहवा ही चलने लगी। लढ़िये की तरह।
लढ़िये की ये खासियत है कि वह ज़रा धीमे चलती है, लेकिन जब एक बार चल पड़ती है तो फिर वह कभी ठहरती नहीं है। बस चलती ही चली जाती है। रेल की तरह उसे कोई बनी-बनाई लीक नहीं चाहिए होती, वह अपने लिए अपनी लीक ख़ुद बना लेती है। इसी खुद बनाई हुई लीक पर वह अनवरत चलती चली जाती है।
तो हिंदी की लढ़िया चलती चली गई और उस पर समय के
साथ-साथ अगल-बगल से कई लद्दू लटकते और चढ़ते गए। ये जब तमाम
षड्यंत्रों के बावजूद हिंदी की लढ़िया रोक नहीं सके.. कुल मिलाकर जो कर सके वह केवल
यह कि
पहले पीछे-पीछे दौड़े, फिर दया की भीख माँगकर लटक गए और जब लटकने की अनुमति मिल गई तो धीरे
से चढ़ गए और फिर असली गाड़ीवानों को जैसे-तैसे आधा-तीहा निपटाकर गाड़ी पर काबिज हो
गए।
बीसवीं सदी में जब हिंदी के नए पाठक ने आँखें खोलीं तो पाया कि हिंदी के पर्चे में बस हिंदी छोड़कर बाकी सब है। अब यह पर्चा चाहे साहित्य का हो, चाहे पत्रिका का, चाहे सिनेमा या संगीत का और चाहे समाचार-पत्र का। पहले हिंदी के अखबारों ने हिंदी छोड़ी.. और यह हिंदी छुड़ाने वाले किसी एक भी अखबार के मालिक नहीं थे। हिंदी के अखबार से हिंदी छुड़ाने वाले केवल और केवल वे स्वनामधन्य हिंदी के संपादक थे जो हिंदी के घर में घुसे ही थे डकैती करने। जिनकी समझ के अनुसार हिंदी का सामान्य पाठक तसव्वुर, परस्तिस, तख़य्युल और इबादत तो समझ सकता था लेकिन प्रामाणिक, अर्चना, अध्यवसाय और आराधना उनके लिए विदेशी शब्द थे। जिनकी समझ से हिंदी का पाठक डिबेट तो समझ सकता था, लेकिन बहस कतई नहीं। खेल गए दिनों की बात हो गया, उसकी जगह स्पोर्ट्स ने ले ली। धन की जगह विधिवत मनी, वित्त की जगह फिनांस, व्यापार की जगह बिज़नस, समाचार की जगह न्यूज़ और स्वास्थ्य की हेल्थ को गड़ासा-बल्लम लेकर कब्जा कराया गया।
जल्दी ही एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आई। उसमें पत्रकारों के नाम पर शुरुआत में ही कुछ बड़े पेंदीविहीन लोटे भर दिए गए और उन्होंने आगे सिर्फ वही भरने की उदात्त परंपरा कायम की। [मेरा यह आशय बिलकुल नहीं कि सब लोटे और बेपेंदी ही हैं। कुछ गैर लोटे और पेंदीदार भी हैं.. लेकिन वे किसी न किसी गलतफहमी के ही नतीजे हैं, रेगुलर नहीं] बेचारे बेपेंदी के लोटों का कभी कोई दोष हुआ है, न होगा। उन्होंने तो बस वही किया जो करने के लिए उन्हें रखा गया था।
अब जब हम नज़र डालते हैं हिंदी की बाल-पत्रिकाओं पर तो देखते हैं कि घर में 21वीं सदी का जो बच्चा दिन-रात नोबिता, शिन्चान, हग्गेमारू, गुड्डू, ऑगी, छोटा भीम, कितरेतसू देख रहा है, पत्रिकाएं उसे बोधकथाओं का परी कोणात्मक रूपांतर परोस रही हैं। वे घर में खुद भी बैठकर हैरी पॉटर का पूरा सिरीज़ तो देख लेंगे और उसकी भूरी-भूरी से लेकर पीली-पीली तक प्रशंसा भी कर देंगे, उसमें वे नए-नए अभिप्राय भी ठूँस देंगे जो थे ही नहीं, लेकिन देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता संतति पर चार लाइन लिखने में उनका ईमान चला जाएगा। वह चंद्रकांता संतति और भूतनाथ जिसे पढ़ने के लिए करोड़ों लोगों ने हिंदी सीखी थी। वही हिंदी जिसकी पीठ पर सवार होकर आज वे विदेशयात्राएं कर रहे हैं।
आलोचना केवल आचार्य शुक्ल को गरिया कर पवित्र हो रही है। उस आचार्य शुक्ल को जिसने हिंदी के साहित्य को उसका व्याकरण और सौंदर्य शास्त्र दिया है। कविता की हालत यह है कि कबीर से लेकर तुलसी तक के सांप्रदायिक कोण तलाशे जा रहे हैं और यह सब वही लोग कर रहे हैं जो दुनिया के सारे मंचों पर सांप्रदायिकता के घोर विरोधी हैं और सच यह है कि इन्हें दूर से देखते ही सांप्रदायिकता की बाँछें खिल जाती हैं। ये न हों तो 22वीं सदी तक सांप्रदायिकता बचे ही नहीं। वह तो राहत की साँस ही तब लेती है जब ये उसके विरोध का प्रहसन करने आ जाते हैं।
ओह, बात तो हो रही थी समाज को बचाने में साहित्य की भूमिका और उसके दंभ की! समाज का आलम यह है कि पश्चिम के जिस समाज में इतना भी नैतिक साहस नहीं है कि वह ईसा से केवल पाँच सौ साल पहले के अपने इतिहास की आँखों में आँखें डालकर देख सके और वह तो छोड़िए आधुनिक काल में जहाँ अभियान चलाकर डाइन होने के नाम लाखों औरतें बाकायदा कोर्ट के निर्देश पर ज़िंदा फूँकी गई हों... उस पश्चिम ने अपनी कालिख हमारे मुँह में पोतने के षड्यंत्र रचे। उन षड्यंत्रों के अब पूरी तरह झूठे और षड्यंत्र सिद्ध हो चुके होने के बावजूद भाई लोग इसी ज़िद पर अड़े हैं कि अगर समाज उस कालिख को अपने मुँह पर नहीं रहने देगा तो हम उसे अपने मुँह पर मल लेंगे। समाज ने अगर कहीं साँस लेने के लिए एक छोटा सा छेद बना रखा था तो उसे इन्होंने कभी न भरने वाली दरार बनाकर दम लिया। किसी गलती से या समय के प्रवाह में समय के कपड़ों में अगर ज़रा सा चीरा कहीं लग गया तो उसे इन्होंने पूरा फाड़ कर ही संतोष किया।
हिंदी की छाती पर आज काबिज विद्वानों की हिंदी समाज को बचाने में यही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका और यही सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। अब अगर केवल अपने और अपने गिरोह के लिखे हुए साहित्य को ही दुनिया का सबसे महान साहित्य कहने और एक समग्र समाज को खंड-खंड करके दिखाने से ही किसी भाषा और साहित्य और उसके कब्जेदारों का कभी भला हुआ हो तो इन कब्जेदारों को भी पूरी उम्मीद बनी रहनी चाहिए।
[दोनों चित्र साभार: गूगल]
#आ_साँड़_तुझे_औकात_बताऊँ
#Hindi #Language
#Literature #Constitution #Assembly #Media #Magazines




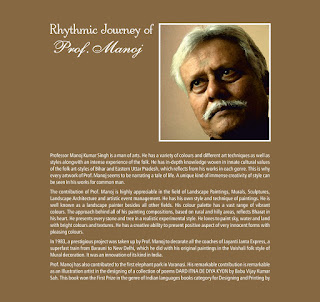


सुन्दर
ReplyDeleteहिंदी की छाती पर आज काबिज विद्वानों की हिंदी समाज को बचाने में यही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका और यही सबसे महत्वपूर्ण योगदान है।